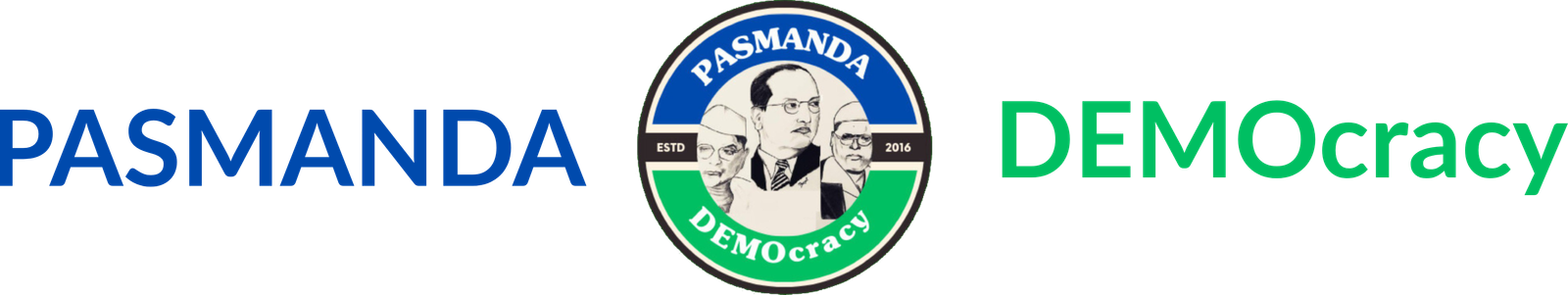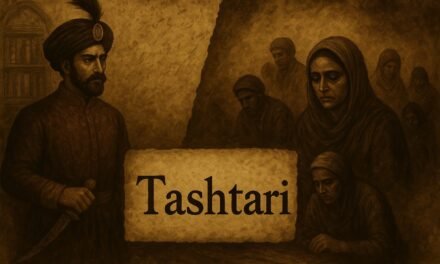~ डॉ. उज्मा ख़ातून
कर्बला का हादसा इस्लामी तारीख़ का एक बहुत अहम मोड़ है। यह सिर्फ़ एक जंग नहीं थी, बल्कि इंसाफ़, सच्चाई और सही क़यादत (नेतृत्व) की लड़ाई थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी (10 अक्टूबर 680 ईस्वी) को कर्बला (आज का इराक़) के रेगिस्तान में हज़रत मुहम्मद ﷺ के नवासे इमाम हुसैन (अ.स.) और उनके 70 से ज़्यादा साथियों को यज़ीद की फ़ौज ने शहीद कर दिया। यह टकराव निजी दुश्मनी नहीं था, बल्कि यह फ़ैसला करने की लड़ाई थी कि इस्लामी रहनुमाई (लीडरशिप) इंसाफ़ और मशवरे (परामर्श) पर होनी चाहिए या बादशाही और ज़ुल्म पर।
इसको समझने के लिए हमें उस दौर की पृष्ठभूमि देखनी होगी। तीसरे ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान (र.अ.) के ज़माने में उन पर इल्ज़ाम लगे कि वो अपने ख़ानदान बनी उमय्या को सरकारी ओहदे दे रहे हैं। इससे लोगों में नाराज़गी फैली और आख़िरकार 656 ईस्वी में उन्हें बग़ावती लोगों ने क़त्ल कर दिया। इसके बाद हज़रत अली (र.अ.) को चौथा ख़लीफ़ा चुना गया। लेकिन शाम के गवर्नर मुआविया(र.अ.)—जो उसी बनी उमय्या क़बीले से थे—ने अली की ख़िलाफ़त को नहीं माना और पहले उस्मान के क़ातिलों से इंसाफ़ की मांग की। इससे जंगे-जमल और सिफ़्फ़ीन जैसी जंगें हुईं, जिसे पहली फ़ितना (गृहयुद्ध) कहा जाता है।
आख़िरकार मुआविया ने सियासी ताक़त हासिल कर ली और हज़रत हसन से सुलह कर ली, जिसमें यह तय हुआ कि मुआविया के बाद वह किसी को अपना जानशीन (उत्तराधिकारी) नहीं बनाएंगे। मगर मुआविया ने इस वादे को तोड़ा और अपने बेटे यज़ीद को ख़लीफ़ा बना दिया—जो इस्लामी रिवायतों के ख़िलाफ़ था, जहां शूरा (मशवरे) से ख़िलाफ़त तय होती थी। जब यज़ीद हुक्मरान बना, तो उसने इमाम हुसैन से बैअत (वफ़ादारी) मांगी। लेकिन इमाम हुसैन ने इंकार कर दिया क्योंकि वो यज़ीद को फ़ासिद और नालायक समझते थे। इराक़ के लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखकर कूफ़ा बुलाया। जब वो अपने अहले-ख़ानदान के साथ वहाँ जा रहे थे, तो यज़ीद की फ़ौज ने कर्बला में उन्हें रोक दिया, पानी बंद कर दिया और 10 मुहर्रम को उन्हें शहीद कर दिया।
इमाम हुसैन की शहादत के बाद, उनके अहले-ख़ानदान को गिरफ़्तार करके कूफ़ा और दमिश्क की गलियों में घुमाया गया, ताकि यज़ीद की ताक़त दिख सके। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ—लोगों की हमदर्दी इमाम हुसैन के साथ हो गई। उस वक़्त मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने पहले ही यज़ीद की हुकूमत को ठुकरा दिया था और अपनी क़यादत का ऐलान कर दिया था। कर्बला के बाद, मक्का, मदीना और दीगर इस्लामी इलाक़ों में यज़ीद के ख़िलाफ़ बग़ावतें बढ़ गईं। यह दौर (683–692 ईस्वी) दूसरी फ़ितना कहलाता है। हालांकि बनी उमय्या कुछ समय और हुकूमत में रहे, लेकिन उनकी नैतिक ताक़त टूट चुकी थी।
बनी उमय्या ने अपनी हुकूमत को नए तरीक़े से संगठित किया—मारवानी शाखा के ज़रिए। ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कई इस्लाही क़दम उठाए जैसे सिक्कों को एक जैसा करना, डाक व्यवस्था और प्रशासनिक केंद्रीकरण। मगर इन सुधारों के बावजूद ग़ैर-अरब मुसलमानों (मवाली) को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा। ख़ुरासान और इराक़ जैसे इलाक़ों में नाराज़गी बढ़ती गई। लोगों को लगने लगा कि बनी उमय्या सिर्फ़ अपने क़बीले को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इंसाफ़ और बराबरी को नजरअंदाज़ करते हैं।
इस असंतोष की वजह से अब्बासी तहरीक उठी। अब्बासी अपने को हज़रत अब्बास (पैग़ंबर ﷺ के चाचा) की औलाद बताते थे। ख़ुरासान में अबू मुस्लिम नामी नेता ने इस तहरीक को संगठित किया। उनका पैग़ाम कर्बला की त्रासदी पर आधारित था। उन्होंने कहा कि वो इमाम हुसैन का बदला लेंगे और सच्चा इस्लामी निज़ाम बहाल करेंगे। उनका नारा था: “अल-रिज़ा मिन आले-मुहम्मद”—यानी पैग़ंबर के घराने से चुना गया शख़्स। उन्होंने अपने मिशन को कर्बला की याद और इंसाफ़ की पुकार से जोड़ा।
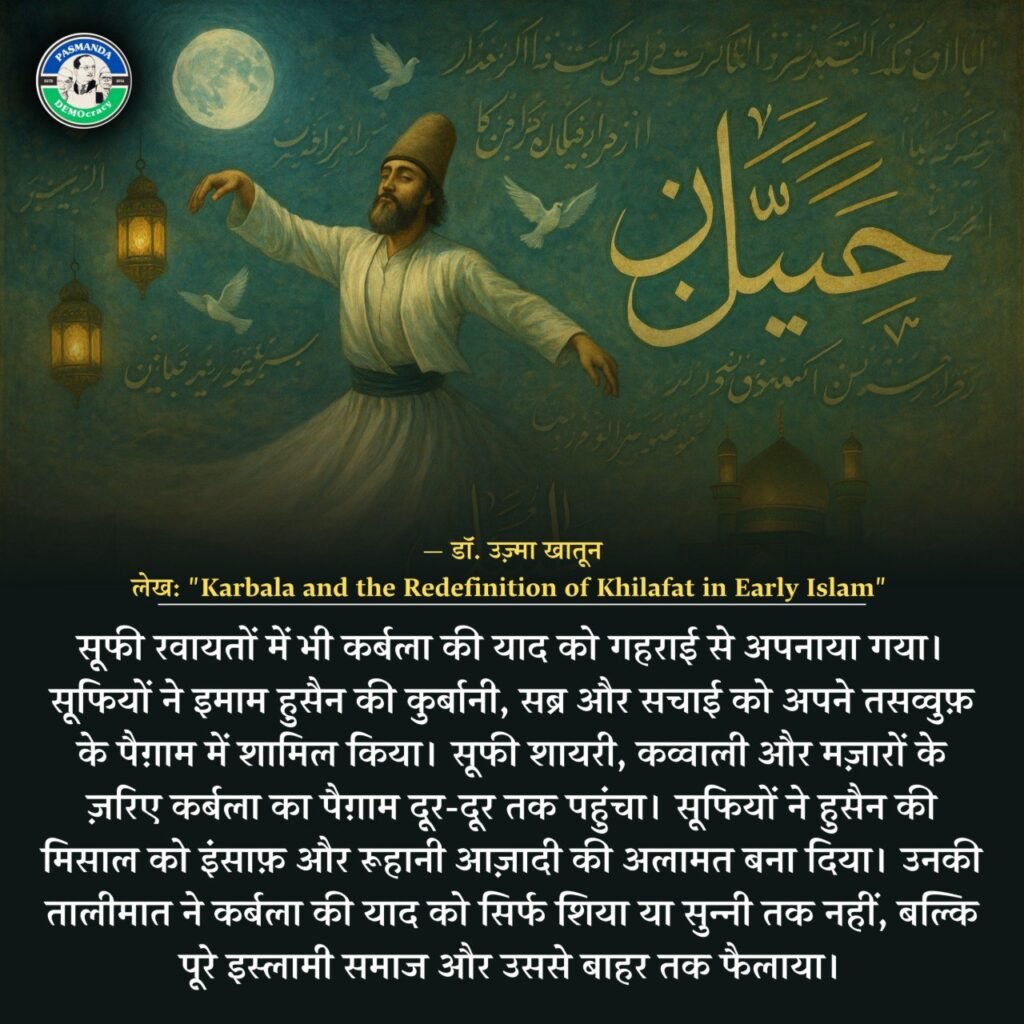
कर्बला का दुख केवल एक सदमा नहीं था, यह बनी उमय्या की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख देने वाला वाक़िआ था। क्योंकि बनी उमय्या ने अपनी हुकूमत को जायज़ ठहराने के लिए कोई मज़हबी बुनियाद नहीं रखी थी, इसलिए जब अब्बासियों ने सरकारी सतह पर एक ज़बरदस्त प्रचार मुहिम चलाई जिसमें कर्बला को ज़ुल्म की मिसाल बताया गया, तो बनी उमय्या कुछ नहीं कह सके। जब उन्होंने यह कहा कि “कर्बला का वाक़िआ तो अल्लाह की मर्ज़ी थी”, तो मशहूर आलिम हसन अल-बसरी ने जवाब दिया, “अल्लाह ज़ुल्म का हुक्म नहीं देता, बल्कि नेकी का हुक्म देता है।” इस जवाब ने एक बुनियादी बात को साफ़ किया—इंसान को नेकी या बदी के चुनाव की आज़ादी है, और हाकिमों को अपने अमल का हिसाब देना होगा। कर्बला ने बनी उमय्या की नैतिक हैसियत छीन ली और अब्बासियों के लिए रास्ता साफ़ किया।
750 ईस्वी में, अब्बासियों ने ज़ाब नदी की लड़ाई में आख़िरी उमय्या ख़लीफ़ा को हरा दिया। ख़िलाफ़त की राजधानी दमिश्क से बग़दाद शिफ्ट हो गई। शुरूआती दौर में अब्बासी हुकूमत ने ग़ैर-अरब मुसलमानों को ज़्यादा हक़ दिए, उलेमाओं की सरपरस्ती की और खुद को अहले-बैत के हिमायती के रूप में पेश किया। मुहर्रम के महीने में उन्होंने मजलिसें, मर्सिए और इमाम हुसैन की याद में जलसे करने की इजाज़त दी। मगर वक़्त के साथ अब्बासी भी केंद्रीकरण और बादशाही की तरफ़ बढ़ गए। उन्होंने भी शिया रस्मों पर पाबंदी लगाई जब उन्हें बग़ावत का डर हुआ। इससे पता चलता है कि तख़्त बदल जाए, लेकिन इख़्तिलाफ़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं बदलती।
शिया सोच में ख़िलाफ़त का मतलब हमेशा हज़रत अली के घराने, ख़ासकर इमाम हुसैन की नस्ल से रहा है। शिया मानते हैं कि सच्चा रहनुमा सिर्फ़ अहले-बैत से हो सकता है—यानि हज़रत अली, बीबी फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। उनका यह भी अकीदा है कि अहले-बैत पाक और मासूम होते हैं। इस तरह शिया भी ख़िलाफ़त को एक ख़ास ख़ानदान तक सीमित मानते हैं। वो बनी उमय्या की बादशाही का विरोध करते हैं, लेकिन ख़ुद भी एक तयशुदा नस्ल की हुकूमत को जायज़ समझते हैं। आज भी बहुत से शिया मानते हैं कि रहनुमाई सिर्फ़ इमाम हुसैन की औलाद में होनी चाहिए। यह मोहब्बत और अकीदत से पैदा हुआ अकीदा, सियासी इख़्तियार को पाक मक़सद का रूप भी देता है।
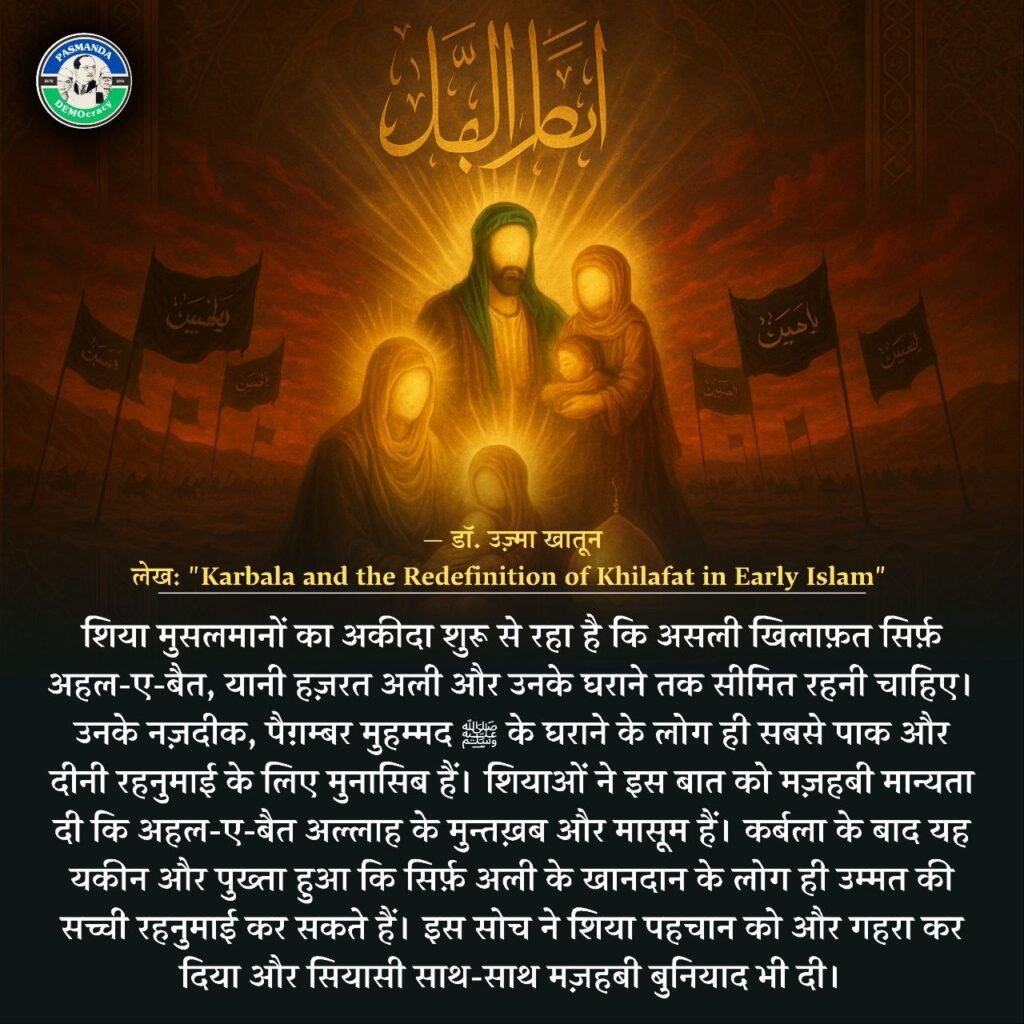
कर्बला के बाद शिया-सुन्नी तफ़रीक़ और वाज़ेह हो गई। पहले इख़्तिलाफ़ सियासी थे, मगर अब मज़हबी शक्ल इख़्तियार कर गए। शियाओं ने इमाम हुसैन और अहले-बैत की क़यादत को अपना ईमानी मरकज़ बना लिया। वहीं सुन्नी मानते रहे कि रहनुमाई किसी भी सलाहियत वाले इंसान को शूरा से मिल सकती है, न कि सिर्फ़ पैग़ंबर के ख़ानदान से। कर्बला शियाओं के लिए एक शहादत और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ अलामत बन गई, जब कि सुन्नियों ने इसे अलग अंदाज़ में याद किया। यही याद का फ़र्क़, एहसास का फ़र्क़ और अक़ीदे का फ़र्क़ इस्लाम के दो रास्तों की बुनियाद बन गया।
कर्बला की याद सिर्फ़ शिया सोच में नहीं, बल्कि सूफ़ी और सुन्नी रिवायतों में भी ज़िंदा रही। शियाओं के लिए ये ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ की पहचान बनी, और हर साल मुहर्रम में वो इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। सूफ़ियों ने भी इमाम हुसैन की सच्चाई, सब्र और रूहानी हिम्मत को सराहा। हालांकि सूफ़ीमत कर्बला के फ़ौरन बाद शुरू नहीं हुई, मगर बाद की सूफ़ी तालीमात में इमाम हुसैन को बहुत इज़्ज़त दी गई। सियासत में भी कर्बला की याद को मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया। उमय्या ने इसे बग़ावत बताया, अब्बासियों ने इसे ज़ालिमों का ज़ुल्म कहा, और सफ़वी शिया सल्तनत ने इसे अपनी पहचान और जواز का ज़रिया बनाया। मगर इन सब के बावजूद, कर्बला का असली पैग़ाम यही रहा: चाहे ज़ालिम कितना भी ताक़तवर क्यों न हो, सच्चाई और इंसाफ़ का साथ देना ही सबसे बड़ा काम है—चाहे उसकी क़ीमत जान ही क्यों न हो।
कर्बला सिर्फ़ एक तारीखी वाक़िआ नहीं था। इसने इस्लामी समाज की रूह को बदल डाला। इसने दिखा दिया कि हक़ीक़ी इख़्तियार ताक़त से नहीं, बल्कि इंसाफ़, अख़लाक़ और अवाम की मर्ज़ी से आता है। कर्बला का सबक़ आज भी लोगों को हौसला देता है—कि ज़ुल्म के नीचे जीने से बेहतर है इज़्ज़त से मरना। यही वजह है कि 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन की कहानी ज़िंदा है—सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो सच्चाई, इंसानियत और इज़्ज़त के लिए खड़ा होता है।
यह लेख आवाज़ थे वॉइस वेबसाइट पर “Karbala and the Redefinition of Khilafat in Early Islam” इस नाम से प्रकाशित हो चूका है
डॉ. उज्मा ख़ातून ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज़ विभाग में पढ़ाया है।