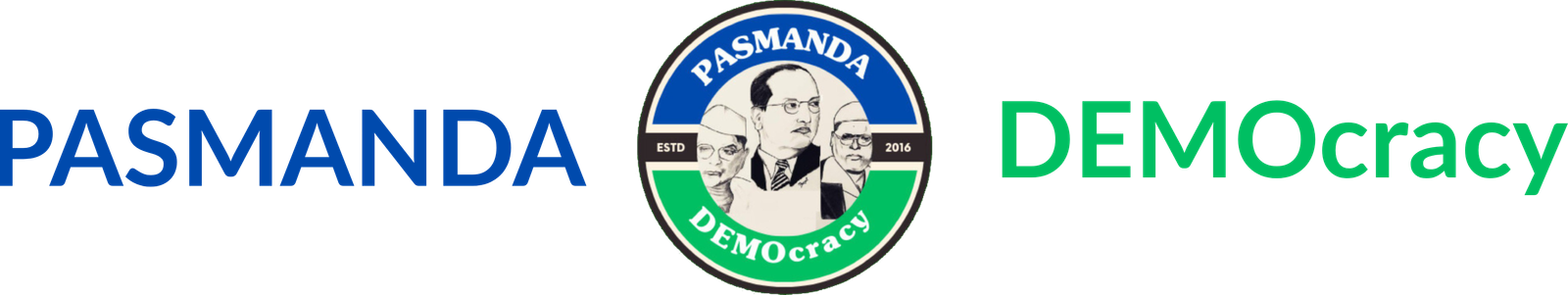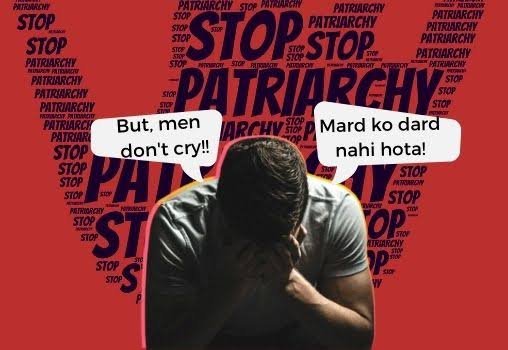लेखक: अब्दुल्लाह मंसूर
हमारे समाज में बहुत पुरानी एक सोच चली आ रही है, जिसमें मर्दों को औरतों से बड़ा, ताकतवर और अहम समझा जाता है। इस सोच को ही पितृसत्ता या पेट्रिआर्की कहा जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है — ऐसा समाज जहाँ हर जरूरी और अहम फैसला मर्द ही करता है और औरत की राय को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। यह केवल किसी एक आदमी की सोच नहीं होती बल्कि पूरे समाज में एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें लड़कों को ‘हुक्म देने वाला’ और लड़कियों को ‘हुक्म मानने वाली’ समझा जाता है।
अगर हम इंसानी समाज के इतिहास को ध्यान से देखें तो यह समझ में आता है कि पितृसत्ता की जड़ें उस वक़्त से शुरू हुईं जब इंसान ने खेती करना और ज़मीन पर मालिकाना हक़ जमाना शुरू किया। पुराने ज़माने में जब इंसान शिकारी जीवन जीता था तब मर्द और औरत दोनों मिलकर काम करते थे, दोनों के बीच बराबरी थी, दोनों साथ में जंगल में खाना ढूंढते, शिकार करते और परिवार चलाते थे। लेकिन जैसे ही खेती और ज़मीन पर कब्ज़े का दौर शुरू हुआ, सारा आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण मर्दों के हाथ में चला गया। मर्दों ने यह तय करना शुरू कर दिया कि घर में किसको क्या मिलेगा, कौन कैसा काम करेगा। धीरे-धीरे औरतों को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया। उनका काम बस बच्चों को पालना, घर सम्भालना और खाना पकाना रह गया। इस तरह पितृसत्ता धीरे-धीरे समाज का हिस्सा बन गई।
आज भी हम अपने आसपास इस सोच के कई उदाहरण रोज़ाना देखते हैं। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है, तो बेटा होने पर पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, जबकि बेटी के जन्म पर अक्सर लोगों का चेहरा उतर जाता है। शादी के समय लड़के की पढ़ाई, नौकरी और कमाई को बहुत अहमियत दी जाती है, और लड़की के लिए यह मान लिया जाता है कि उसका असली मकसद सिर्फ सुंदर दिखना और घर सम्भालना है। स्कूलों में लड़कों को साइंस, टेक्नोलॉजी और गणित में आगे बढ़ाया जाता है, वहीं लड़कियों से कहा जाता है कि तुम्हें तो आखिर में घर ही सम्भालना है। ऑफिसों में भी यह फर्क साफ नजर आता है, एक ही काम करने पर भी मर्दों को ज्यादा वेतन मिलता है और उन्हें ऊँचा पद भी जल्दी दे दिया जाता है। यह सब बातें इस बात का सबूत हैं कि पितृसत्ता आज भी हमारे जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है।
जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो अक्सर यह समझा जाता है कि यह सोच औरतों को ही कमजोर बनाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यवस्था मर्दों को भी बुरी तरह प्रभावित करती है।
बेल हुक नाम की लेखिका ने अपनी किताब ‘द विल टू चेंज: मेन, मस्कुलिनिटी, एंड लव’ में यह बहुत खूबसूरती से समझाया है कि पितृसत्ता पुरुषों से सबसे पहले जो हिंसा करवाती है, वो दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ही होती है। समाज मर्दों से यह मांग करता है कि वो अपने दिल और मन की भावनाओं को मार डालें।
मर्दों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि रोना, डरना, नर्मी दिखाना या प्यार जताना कमजोरी की निशानी है। एक ‘असली मर्द’ हमेशा सख्त, मजबूत और बेपरवाह दिखता है।
यह सब सीखते-सीखते एक मासूम बच्चा धीरे-धीरे अपने असली जज्बातों को छुपाना शुरू कर देता है। जब भी कोई लड़का गिरकर रोता है, तो उसे कहा जाता है — “क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो?” अगर कोई लड़का अपने दोस्त से अपने डर या दुख की बात करता है, तो समाज उसे कमज़ोर समझता है। उसकी नर्मी और संवेदनशीलता को ‘कमजोरी’ का नाम दे दिया जाता है। इस तरह पितृसत्ता एक बच्चे की मासूमियत और उसकी इंसानियत को दबा देती है। वह बच्चा धीरे-धीरे खुद को ऐसा इंसान बनाता है जो बाहर से सख्त दिखे लेकिन अंदर से अकेला, डरा हुआ और भावनात्मक रूप से टूट चुका हो।
पितृसत्ता मर्दों की सेहत पर भी असर डालती है। मर्दों को यह सिखाया जाता है कि अगर वो बीमार हैं या थके हुए हैं, तो भी उन्हें मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मदद मांगना कमजोरी मानी जाती है। इस वजह से बहुत से मर्द बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते और कई बार खतरे में पड़ जाते हैं। यही सोच उन्हें अपनी जिंदगी में कई बार बेवजह जोखिम उठाने के लिए मजबूर करती है ताकि वो यह साबित कर सकें कि वो बहादुर और असली मर्द हैं।
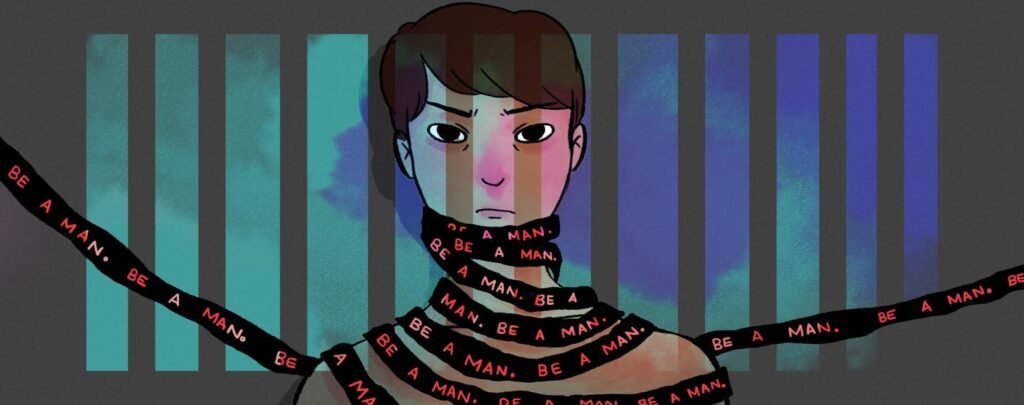
पितृसत्ता न सिर्फ मर्द की भावनाओं को मारती है, बल्कि उसकी ज़िंदगी की अहमियत को भी कम करके देखती है। अगर हम फिल्मों पर नज़र डालें तो आमतौर पर पितृसत्ता से जुड़े स्टीरियोटाइप हमारी आँखों के सामने आते हैं। भारतीय संदर्भ में ‘एनिमल’ और ‘कबीर सिंह’ जैसी फिल्मों में टॉक्सिक मर्दानगी को ग्लोरिफाई करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मर्द गुस्सैल, हिंसक और दूसरों पर हुक्म चलाने वाला बनकर सामने आता है। पर इन फिल्मों में एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जो अक्सर चर्चा से गायब रहती है — मर्दों की जान और भावनाओं की कोई क़ीमत नहीं दिखाई जाती। जैसे उनका जीवन और जज्बात दोनों ही कमतर हैं। मर्दों को एक मशीन की तरह दिखाया जाता है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो दर्द सहें, मरें-खपें लेकिन कभी शिकायत न करें।
अगर हम और ध्यान से फिल्मों की तरफ देखें तो यह बात और साफ़ होती है। ‘टाइटैनिक’ फिल्म में एक सीन में जहाज डूब रहा होता है। उस वक्त औरतों और बच्चों को सबसे पहले बचाया जाता है और मर्दों को मौत के हवाले छोड़ दिया जाता है। भले ही हर इंसान अपनी जान से बराबर प्यार करता है, लेकिन समाज यह तय कर देता है कि मर्दों की जान की क़ीमत सबसे कम है। इस सोच के चलते मर्दों से उम्मीद की जाती है कि वो हर हाल में खुद को कुर्बान कर दें, चाहे उनका मन कितना भी दुखी या डर से भरा क्यों न हो।
पितृसत्ता मर्दों की दोस्ती और रिश्तों को भी कमजोर कर देती है। जब समाज किसी मर्द को सिखाता है कि वह अपने जज्बातों को छुपाए और हमेशा सख्त बने, तो वह अपने दोस्तों से भी दिल की बातें नहीं कर पाता। अगर कोई दोस्त परेशानी में है, तो उसे भी बस यही सिखाया गया होता है कि “सब ठीक है” कहकर चुप रहना है। ऐसे में मर्दों की दोस्ती सतही रह जाती है, गहरी और सच्ची दोस्ती बन ही नहीं पाती। दूसरा नुकसान यह होता है कि मर्दों के बीच हमेशा एक किस्म की प्रतियोगिता बनी रहती है। हर मर्द दूसरे से बेहतर दिखने, ज्यादा ताकतवर बनने और ज्यादा सफल होने की कोशिश में जुटा रहता है। इस वजह से दोस्ती में भी ईमानदारी और अपनापन खत्म हो जाता है।
पितृसत्ता ने मर्दों को सिर्फ भावनाओं से नहीं, रिश्तों से भी काट दिया है। जब मर्द अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे न सिर्फ खुद से दूर हो जाते हैं, बल्कि अपने परिवार से भी। एक बाप अपने बेटे से दिल खोलकर प्यार नहीं कर पाता, एक बेटा अपने पिता से अपने डर या सपने शेयर नहीं कर पाता। एक पति अपनी पत्नी से अपने मन की बातें कह नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी मर्दानगी कम हो जाएगी। इस तरह पितृसत्ता एक इंसान के दिल को अकेला कर देती है, और ये अकेलापन उसे गुस्सैल, तनावग्रस्त और उदास बना देता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि पितृसत्ता मर्दों के दिमाग में यह भर देती है कि उनकी असली पहचान उनकी सख्ती और गुस्से में छुपी है। जब कोई मर्द दुखी होता है, डरता है या तनाव में होता है, तो उसे यह समझाया गया होता है कि इन सब जज्बातों को सिर्फ गुस्से के जरिये ही बाहर निकाला जा सकता है। इस वजह से वो अपने गुस्से का शिकार खुद भी होता है और उसके परिवार के लोग भी। ऑफिस में दिक्कत हो तो वो घर आकर बच्चों पर चिल्लाता है। अपनी बीवी से प्यार जताने की जगह उससे दूरी बना लेता है। धीरे-धीरे यह दूरी रिश्तों को तोड़ देती है और इंसान और भी अकेला हो जाता है।
बेल हुक ने सही ही कहा है कि “पितृसत्ता मर्दों से उनकी इंसानियत छीन लेती है।” समाज ने मर्दों को ऐसा बना दिया है जो अपनी असली फितरत को छुपाता है। उसे यह बताया गया है कि ताकत ही सब कुछ है, और भावनाएं कमजोरी हैं। जबकि हकीकत यह है कि भावनाएं ही इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर कोई मर्द अपने बच्चों से प्यार जताए, अपने दोस्त से अपना दुख साझा करे या अपनी थकान और डर को खुलकर बोले तो यह उसकी इंसानियत की पहचान है, न कि कमजोरी।
अगर हम चाहते हैं कि समाज बेहतर बने तो हमें पितृसत्ता के इस ढांचे को समझना और तोड़ना होगा। हमें यह मानना होगा कि मर्द भी पितृसत्ता के शिकार हैं। हमें मर्दों को यह सिखाना होगा कि भावनाएं छुपाना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने दिल की बात कहना हिम्मत का काम है। जब मर्द खुद से जुड़ पाएंगे, अपने जज्बातों को समझ पाएंगे, तो वो अपने रिश्तों में भी सच्चाई और अपनापन ला पाएंगे।
सिमोन द बोवोआर ने एक बार कहा था कि औरत पैदा नहीं होती, उसे समाज बनाता है। उसी तरह मर्द भी पैदा नहीं होते, समाज उन्हें गढ़ता है।
इसलिए अगर हम एक बेहतर और इंसानी दुनिया चाहते हैं तो हमें पितृसत्ता की इस सोच को खत्म करना ही होगा। जब मर्द और औरत दोनों बराबरी के साथ, अपने असली जज्बातों को पहचान कर, खुलकर जी पाएंगे तभी समाज में सच्चा बदलाव आएगा।