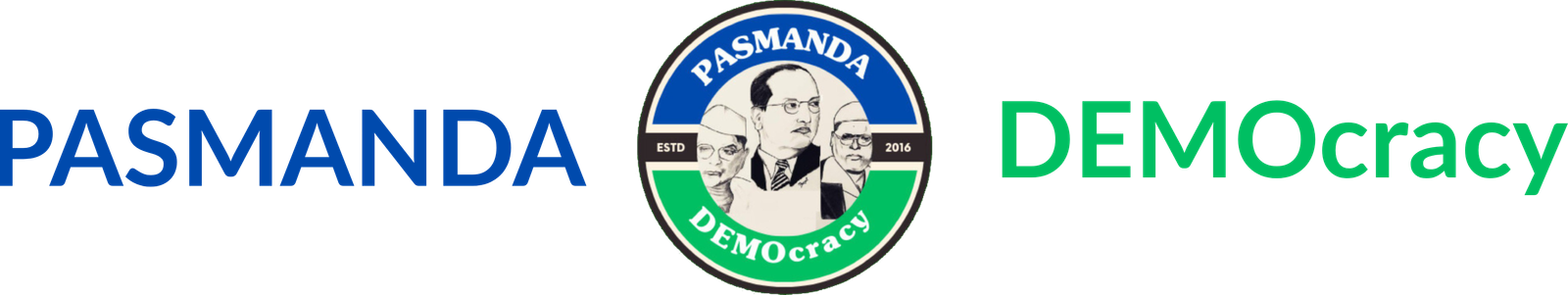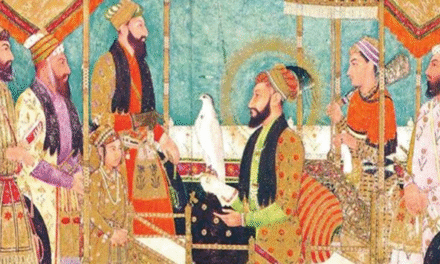लेखक: अब्दुल्लाह मंसूर
दक्षिण एशिया में हाल के वर्षों में युवाओं के आंदोलनों ने राजनीतिक स्थिरता को गहराई से चुनौती दी है। श्रीलंका में अप्रैल 2022 में महंगाई और आर्थिक संकट से उपजे प्रदर्शन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे तक पहुँच गए। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में रोजगार कोटे के खिलाफ छात्र आंदोलन ने हिंसक रूप लिया और बड़ी संख्या में मौतों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। नेपाल में सितंबर 2025 में जनरेशन-ज़ेड के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ, वह राजनीतिक बदलाव तक जा पहुँचा। इन घटनाओं ने यह दिखा दिया कि दक्षिण एशिया के युवा वर्ग केवल स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ साझा चेतना के साथ खड़े हो रहे हैं।
नेपाल का यह उभार महज राजनीतिक संकट नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही व्यवस्थागत विफलताओं का नतीजा है। लोकतांत्रिक ढांचे में संक्रमण के बावजूद भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बेरोजगारी ज्यों की त्यों बनी रही। 1990 के बाद राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ने की प्रक्रिया उम्मीदें जगाती थी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने आम जनता की समस्याओं को दरकिनार कर दिया। माओवादी विद्रोह, बार-बार सरकार बदलना और नेताओं का अपने परिवारों को केंद्र में रखना लोगों की निराशा को और गहराता गया।
इस पृष्ठभूमि में जनरेशन-ज़ी सामने आई। यह वह पीढ़ी है जिसने डिजिटल युग में पलकर राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। इनके लिए भ्रष्टाचार, असमानता और सत्ता का वंशवाद स्वीकार्य नहीं था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर “नेक्स्ट जेनरेशन नेपाल” जैसे पेजों ने इस असंतोष को संगठित रूप दिया। “नेपो किड्स” और “नेपो बेबीज़” जैसे शब्द युवाओं की झुंझलाहट के प्रतीक बन गए। हालात तब और बिगड़े जब सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। इसे युवाओं ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना और सड़कों पर उतर आए। पुलिस गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और सरकारी प्रतीकों पर गुस्सा फूट पड़ा। आंदोलन ने सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं बल्कि राज्य की नीतियों को भी कठघरे में खड़ा कर दिया।

युवाओं के इस उभार के साथ नए चेहरे भी सामने आए। काठमांडू के मेयर बालेन शाह और राष्ट्री स्वंतंत्र पार्टी के रवि लामिछाने जैसे नेताओं ने जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को आगे बढ़ाया। बालेन शाह ने युवाओं से हिंसा छोड़कर शांतिपूर्ण बदलाव की अपील की, जबकि राजनीतिक नेतृत्व में हुए इस्तीफों ने यह संकेत दिया कि अस्थिरता के बीच भी लोकतंत्र को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन असली चुनौती संवैधानिक सुधार और संवाद से जुड़ी है, जो दीर्घकालिक स्थिरता ला सके।
नेपाल की यह उथल-पुथल केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत के लिए यह स्थिति चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई। खुली सीमाएँ और सांस्कृतिक समानताएँ दोनों देशों को जोड़ती हैं, लेकिन अस्थिरता का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों तक फैल सकता है। भारत ने अब तक संयम दिखाते हुए नेपाल की संप्रभुता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया है। आक्रामक हस्तक्षेप से बचते हुए उसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग पर ज़ोर दिया है। यह नीति न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम है।
नेपाल की युवा क्रांति के केंद्र में बेरोजगारी, शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे हैं। लाखों नेपाली युवा रोज़गार की तलाश में विदेश जाते हैं, जो भीतर ही भीतर असंतोष का इशारा है। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो अस्थिरता बनी रहेगी। जनसांख्यिकीय लाभ तभी सार्थक होगा जब युवा वर्ग को रचनात्मक दिशा मिले। नेपाल के सामने दो रास्ते हैं। एक ओर वह संवैधानिक सुधार और पारदर्शिता के माध्यम से युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर सकता है। दूसरी ओर मौजूदा ढांचे में अस्थिर और हिंसक संक्रमण का खतरा है। स्थायी भविष्य वही होगा जो युवाओं की आकांक्षाओं को जगह दे और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करे।
बांग्लादेश और नेपाल की स्थितियों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों में आंदोलन युवाओं की असंतुष्टि से उपजे, लेकिन उनके परिणाम अलग-अलग रहे। बांग्लादेश में रोजगार कोटे के खिलाफ आंदोलन ने हिंसा और दमन के बाद अल्पसंख्यकों पर हमलों का रूप ले लिया। सिर्फ 16 दिनों में दो हजार से अधिक घटनाएँ सामने आईं, जिनमें मंदिर, घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हुए और कई निर्दोष मारे गए। यह बताता है कि युवा आंदोलनों के साथ सांप्रदायिक तनाव जुड़ जाने पर स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। वहीं नेपाल में अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, हालांकि यह जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। यही कारण है कि दक्षिण एशिया में ऐसे आंदोलनों को केवल लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में मोड़ना आवश्यक है, न कि उन्हें सामाजिक विभाजन का साधन बनने देना।
नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाकर और नेतृत्व में बदलाव कर यह संकेत दिया है कि वह संकट को शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। आगे का रास्ता संवैधानिक सुधारों, संवाद और जवाबदेही से होकर ही गुजरता है। भारत ने इस दौर में जिस संयम का परिचय दिया है, वह उसकी परिपक्व कूटनीति को दर्शाता है। नेपाल के युवाओं के साथ शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। दक्षिण एशिया में स्थिरता तभी संभव है जब लोकतंत्र का आधार मजबूत हो और क्षेत्रीय साझेदारी विश्वास पर टिकी हो।
नेपाल की युवा क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता का ढांचा अब पुराना नहीं चल सकता। युवा वर्ग सत्ता में जवाबदेही, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की मांग कर रहा है। यह केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं बल्कि लोकतंत्र की नई शुरुआत है। नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका नेतृत्व इस ऊर्जा को किस दिशा में ले जाता है। यदि मूल समस्याओं का समाधान हुआ, तो नेपाल न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए स्थिरता और विकास का उदाहरण बन सकता है। आख़िरकार, यह आंदोलन केवल एक देश की राजनीतिक कहानी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी और अवसर दोनों है। नई पीढ़ी बदलाव की शक्ति बन चुकी है और उसके नेतृत्व में दक्षिण एशिया का लोकतांत्रिक भविष्य तय होगा।
लेखक पसमांदा चिंतक हैं