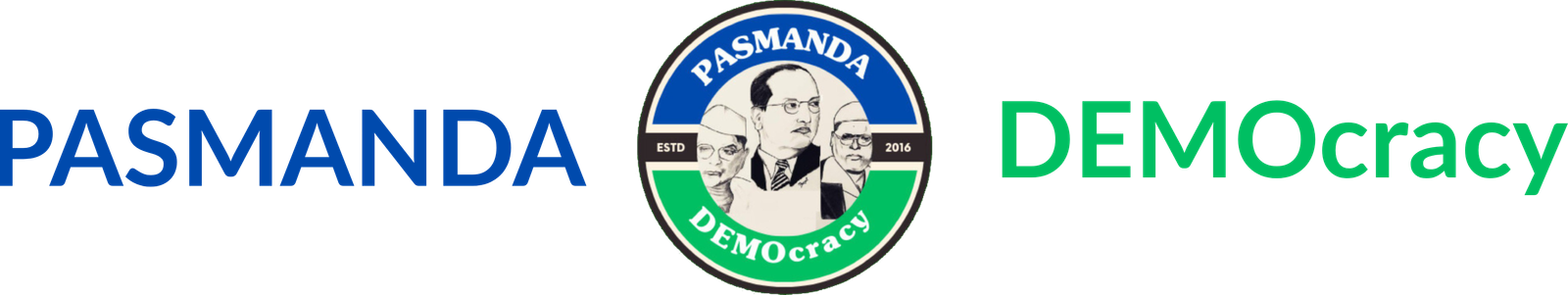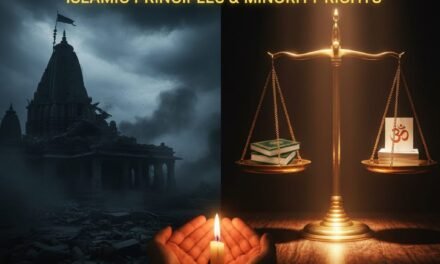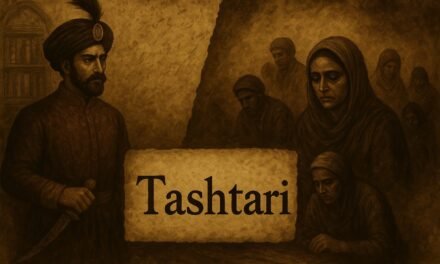- नियामतुल्लाह अंसारी: गुमनाम नायक जिन्होंने जातिगत अन्याय के खिलाफ़ जीती ऐतिहासिक लड़ाई
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले से टूटा सदियों पुराना सामाजिक शोषण
- कांग्रेस और मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े नेता ने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को दी चुनौती
~अब्दुल्लाह मंसूर
भारतीय समाज के इतिहास में जब भी सामाजिक न्याय और समानता की बात होती है, तो अक्सर कुछ बड़े नाम ही हमारी ज़ुबान पर आते हैं। लेकिन इतिहास की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ उन गुमनाम नायकों ने लड़ी हैं, जिनके योगदान को समय की धूल ने धुंधला कर दिया है। ऐसे ही एक महान योद्धा थे श्री नियामतुल्लाह अंसारी, जिन्होंने न केवल भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर गहरे तक पैठी हुई जातिगत भेदभाव और सामंती उत्पीड़न की व्यवस्था को भी चुनौती दी। उनकी कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस लड़ाई की दास्तान है जो दबे-कुचले और हाशिए पर पड़े मुसलमानों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ी गई थी। इस कहानी का केंद्र बिंदु है ‘रज़ालत टैक्स’ नामक वह अपमानजनक कर, जिसने तथाकथित ‘अशरफ़’ (कुलीन) मुसलमानों को ‘अरज़ाल’ (हीन) समझे जाने वाले मुसलमानों का शोषण करने का एक सामाजिक और कानूनी अधिकार दे रखा था। यह लेख श्री नियामतुल्लाह अंसारी के जीवन और उस ऐतिहासिक संघर्ष को समर्पित है जिसने भारतीय मुसलमानों के एक बड़े तबके को सम्मान से जीने का हक़ दिलाया।
श्री नियामतुल्लाह अंसारी 28 सितंबर 1903 में गोरखपुर के एक संपन्न परिवार में जन्मे, नियामतुल्लाह जी का देशप्रेम छोटी उम्र में ही जागृत हो गया था। कलकत्ता में अपनी पढ़ाई के दौरान, वे महज़ 18 साल की उम्र में गांधीजी के 1920 के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर गोरखपुर लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। वे कांग्रेस के एक ज़मीनी और प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने 1925 में कानपुर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और 1936 में उन्हें गोरखपुर शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता के कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया | वे मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति के विरुद्ध एक चट्टान की तरह खड़े रहे। इसके लिए उन्होंने ‘मोमिन कॉन्फ्रेंस’ को अपना मंच बनाया और पिछड़े मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से जोड़ा। 1939 में, अपने ससुर जनाब मुर्तजा हुसैन के संरक्षण में, उन्होंने गोरखपुर में मोमिन कॉन्फ्रेंस के एक सफल अधिवेशन का आयोजन किया। यह वही मोमिन कॉन्फ्रेंस थी जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई और जिसने स्वतंत्रता संग्राम में पूरी मुखरता से भाग लिया। आज़ादी के बाद भी वे राजनीति में सक्रिय रहे और 1962 में गोरखपुर से भारी बहुमत से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। दुर्भाग्य से, वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लकवे की बीमारी के कारण 1970 में उनका निधन हो गया।

लेकिन नियामतुल्लाह अंसारी की पहचान केवल एक स्वतंत्रता सेनानी तक ही सीमित नहीं थी। वे मुस्लिम समाज के भीतर व्याप्त गहरे जातिगत भेदभाव और सामंती शोषण के भी कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ‘रज़ालत टैक्स’ जैसी अपमानजनक प्रथाओं के खिलाफ़ एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीतकर लाखों दबे-कुचले पसमांदा मुसलमानों को सम्मान का अधिकार दिलाया। ‘रज़ालत टैक्स’ को समझने के लिए हमें उस दौर की सामंती और ज़मींदारी व्यवस्था को समझना होगा, जहाँ समाज जाति के आधार पर ‘अशरफ़’ (कुलीन) और ‘अरज़ाल’ (हीन या कमीन) में बंटा हुआ था। ‘अशरफ़’ वर्ग में सैयद, शेख़, मुग़ल, पठान जैसी जातियाँ आती थीं, जो खुद को शासक वर्ग का मानती थीं, जबकि ‘अरज़ाल’ में जुलाहे (बुनकर), क़साई (मांस विक्रेता), राईन (सब्ज़ी विक्रेता), धोबी, नाई जैसे कारीगर और मेहनतकश समुदाय आते थे।
1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भूमि बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत ‘वाजिब-उल-अर्ज़’ नामक दस्तावेज़ तैयार किया गया। यह दस्तावेज़ गाँवों के रीति-रिवाजों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक रिकॉर्ड था। कानूनी तौर पर, इसने ज़मींदारों और ताल्लुकेदारों को भूमि का स्वामी बना दिया और उनके पारंपरिक अधिकारों को एक अर्ध-कानूनी ढाँचा प्रदान किया।हालांकि यह औपचारिक कानून नहीं था, फिर भी इसका प्रभाव व्यापक था। इसी दस्तावेज़ के आधार पर ज़मींदार तथाकथित ‘निम्न’ जातियों से बेगार (बिना मज़दूरी के काम) और कारीगरों से मुफ्त सेवाएँ वसूलने को अपना अधिकार मानते थे। इसमें ‘घरदुआरी’ या ‘परजोट’ जैसे करों का भी उल्लेख था, जो स्पष्ट रूप से केवल ‘रज़ील’ (निम्न) समझी जाने वाली जातियों पर लगाए जाते थे।
ज़मींदार, जो अक्सर ‘अशरफ़’ वर्ग से होते थे, इन ‘अरज़ाल’ जातियों से एक अपमानजनक टैक्स वसूलते थे, जिसे ‘रज़ालत टैक्स’ या ‘घरदुआरी’ कहा जाता था। यह टैक्स इस बात का प्रतीक था कि कर चुकाने वाला व्यक्ति ‘रज़ील’ यानी नीचा है और ज़मींदार ‘शरीफ़’ यानी ऊँचा है। यह सिर्फ़ एक आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि सामाजिक अपमान का एक संस्थागत रूप था। ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने ज़मींदारी अधिकारों के दस्तावेज़, जिसे “वाजिब-उल-अर्ज़” कहा जाता था, में इस तरह के शोषणकारी रिवाजों को कानूनी हक़ के तौर पर दर्ज करवा लिया था। सदियों से दबे-कुचले लोग इसे अपनी किस्मत मानकर यह टैक्स चुकाते आ रहे थे। ऐसे ही माहौल में, गोरखपुर के काज़ी ज़मींदार तसद्दुक हुसैन भी अपने इलाके के ‘रज़ील’ समझे जाने वाले मुसलमानों से यह टैक्स वसूलते थे।
इसी अन्याय के खिलाफ नियामतुल्लाह अंसारी ने अपनी आवाज़ बुलंद की। वे खुद जुलाहा (अंसारी) समुदाय से थे, जिसे ‘अरज़ाल’ की श्रेणी में रखा जाता था। उन्होंने न केवल खुद यह अपमानजनक टैक्स देने से इनकार कर दिया, बल्कि दूसरे पिछड़े समुदायों के लोगों को भी इसे न चुकाने के लिए संगठित किया। यह ज़मींदार की सत्ता को सीधी चुनौती थी। ज़मींदार काज़ी तसद्दुक हुसैन यह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई ‘रज़ील’ उसके हज़ारों साल पुराने अधिकार के खिलाफ़ बगावत करे। उसने नियामतुल्लाह अंसारी पर बकाया टैक्स की वसूली के लिए गोरखपुर की निचली अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। यहीं से उस ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसे “अशरफ़ बनाम अरज़ाल” के नाम से जाना जाता है। यह मुकदमा सिर्फ़ पाँच रुपये कुछ आने का नहीं था, बल्कि यह इस बुनियादी सवाल पर लड़ा गया कि “क्या जुलाहे रज़ील हैं?” यह लड़ाई नियामतुल्लाह अंसारी के सम्मान की नहीं, बल्कि पूरे पसमांदा समाज के स्वाभिमान की लड़ाई थी। उस सामंती दौर में, जहाँ ग़रीबों की कोई आवाज़ नहीं होती थी, ज़मींदारी व्यवस्था के खिलाफ़ खड़ा होना किसी अदम्य साहसी व्यक्ति के ही बस की बात थी।
यह मुकदमा गोरखपुर की अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक लड़ा गया। ज़मींदार पक्ष ने यह साबित करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया कि जुलाहे और अन्य कारीगर जातियाँ ‘रज़ील’ हैं और उनसे ‘रज़ालत टैक्स’ वसूलना उनका पारंपरिक और कानूनी अधिकार है। इस बात को साबित करने के लिए ज़मींदार के बेटे, काज़ी तल्मुज़ हुसैन, जो हैदराबाद में निज़ाम की सरकार में नौकरी करते थे, ने “जुलाहा नामा” नाम की एक अपमानजनक किताब लिखी और उसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया। इस किताब में अंसारी समुदाय को नीचा दिखाने के लिए हर तरह की झूठी दलीलें दी गई थीं। इसके जवाब में, नियामतुल्लाह अंसारी और उनके साथियों ने भी डटकर मुक़ाबला किया। उनकी तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी इस्तफ़ा हुसैन अंसारी और मुस्तफ़ा हुसैन अंसारी जैसे वकीलों ने की। उन्होंने अदालत में “काज़ी नामा” दाखिल किया और इस्लामी सिद्धांतों का हवाला देते हुए यह दलील दी कि इस्लाम में सभी मुसलमान बराबर हैं और किसी भी मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान को ‘रज़ील’ कहकर उससे टैक्स वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। दुख की बात यह है कि कुछ उलेमाओं ने भी इस मामले में ज़मींदार का साथ दिया, लेकिन नियामतुल्लाह अंसारी अपने इरादे पर अडिग रहे। यह मुकदमा “मोमिन गज़ट” जैसे अख़बारों में लगातार छपता रहा, जिससे पूरे देश के मोमिन और पिछड़े समुदायों में एक नई चेतना और जोश पैदा हुआ।
आखिरकार, एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद, अदालत ने ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया। 22 मई, 1939 को अदालत ने यह माना कि जुलाहे ‘रज़ील’ नहीं हैं और ज़मींदार को उनसे ‘रज़ालत टैक्स’ वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। यह सिर्फ़ नियामतुल्लाह अंसारी की जीत नहीं थी; यह उन सभी “रज़ील” समझे जाने वाले मुसलमानों की जीत थी, जिन्हें सदियों से अपमान और गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। इस एक फ़ैसले ने ‘रज़ालत टैक्स’ की प्रथा को समाप्त कर दिया और लाखों दबे-कुचले लोगों को सम्मान के साथ सिर उठाकर जीने का हक़ दिया। यह जीत इस बात का प्रमाण थी कि अगर संगठित होकर संघर्ष किया जाए तो बड़ी से बड़ी सामंती ताक़त को भी झुकाया जा सकता है। इस मुकदमे का एक गहरा राजनीतिक महत्व भी था। यह वह दौर था जब मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसे संगठन मुस्लिम लीग की ‘अशरफ़’ राजनीति को चुनौती दे रहे थे और देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ रहे थे। यह मुकदमा पिछड़े मुसलमानों को हीन भावना में धकेलकर आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करने की एक राजनीतिक साज़िश भी थी, जिसे नियामतुल्लाह अंसारी जैसे नेताओं ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से नाकाम कर दिया।
श्री नियामतुल्लाह अंसारी को दुनिया हमेशा एक “कौम के मसीहा” और एक सच्चे सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में याद रखेगी। उन्होंने उस दौर में ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाई जब ऐसा करने की कल्पना करना भी मुश्किल था। उन्होंने न सिर्फ़ अंग्रेज़ी हुकूमत का मुक़ाबला किया, बल्कि समाज के भीतर मौजूद उन अंग्रेज़ों के वफ़ादारों को भी चुनौती दी जो धर्म और जाति के नाम पर अपने ही लोगों का शोषण कर रहे थे। उन्होंने बुनकर समुदाय और अन्य ‘रज़ील’ कही जाने वाली जातियों को अपमान की बेड़ियों से आज़ाद कराकर समाज में बराबरी का दर्जा दिलाया। आज जब हम सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं, तो हमें श्री नियामतुल्लाह अंसारी के इस अभूतपूर्व योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी विरासत बाद में उनके प्रिय भांजे और तनवीर सलीम के पिता, स्वर्गीय अशफ़ाक़ हुसैन अंसारी को मिली, जिन्होंने उस मशाल को जलाए रखा जिसे उनके मामूं ने रौशन किया था। नियामतुल्लाह अंसारी की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली लड़ाई सिर्फ़ राजनीतिक आज़ादी की नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और समानता की भी होती है, और यह लड़ाई आज भी जारी है।
लेखक पसमांदा चिंतक हैं
संदर्भ
1:-अंसारी, अश्फ़ाक़ हुसैन। (मोमिन कॉन्फ्रेंस की दस्तावेज़ी तारीख)। दिल्ली: मोमिन मीडिया, 2000
2:-सलीम,तनवीर, स्वतंत्रता सेनानी नियामतुल्लाह अंसारी की 110वीं जयंती, सबरंग, 5 अक्टूबर, 2016