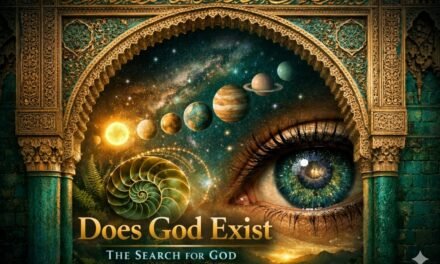उर्दू ज़ुबान में पसमांदा अदब की स्थिति पर विचार करते समय, यह स्पष्ट होता है कि इस साहित्य में पसमांदा समुदाय की आवाज़ें बहुत हद तक दब गई हैं। उर्दू साहित्य पर मुख्यतः अशराफ़ मुस्लिमों का प्रभुत्व रहा है, जो इसे अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वार्थों के लिए उपयोग करते रहे हैं। पसमांदा समुदाय के लेखकों और कवियों ने उर्दू साहित्य में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनके मुद्दे और अनुभव अक्सर मुख्यधारा के साहित्य में अनदेखे रह जाते हैं। जहां दलित साहित्य ने अपनी पहचान बनाई है और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया है, उर्दू ज़ुबान में ऐसा कोई अदब नज़र नहीं आता।
उर्दू साहित्य में पसमांदा अदब की अनुपस्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि उर्दू भाषा को ऐतिहासिक रूप से उच्च वर्गों से जोड़ा गया है। इस कारण, पसमांदा समुदाय के अनुभव और दृष्टिकोण साहित्यिक मंच पर उतनी प्रमुखता से नहीं उभर पाए हैं। इस लेख में हम उर्दू के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, विशेष रूप से यह देखते हुए कि कैसे यह भाषा अशराफ समाज की सभ्यता और संस्कृति का आईना बनी और कैसे इसमें पसमांदा समाज का दर्द अदृश्य रह गया। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि उर्दू को अशराफों ने अपने वर्चस्व के एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया।
उर्दू है जिसका नाम
उर्दू भाषा का इतिहास समृद्ध और जटिल है, जिसमें यह विभिन्न नामों और रूपों से गुजरी है। इसे कभी स्थानीय शब्दों, मुहावरों और उपमाओं से सजी हुई भाषा के रूप में देखा जाता था, जो यहाँ की संस्कृति को परिलक्षित करती थी और आम लोगों की जुबान में शामिल थी। इसे “हिंदवी” भी कहा जाता था। उर्दू, जो आज एक सम्भ्रांत वर्ग की बोली मानी जाती है, ने अपना सफर जबान-ए-हिंद से शुरू किया और विभिन्न नामों जैसे जबान-ए-दिल्ली, रेख़्ता, गुजरी, दक्खनी, और ज़बान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला के रूप में अपने अस्तित्व को स्थापित किया। वैसे उर्दू के रूप में इस भाषा की पहचान 18 शताब्दी के अंत में हुई है। ‘उर्दू’ तुर्की भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शाही सैन्य शिविर या बाज़ार/ तंबू। ज़ाहिर है तुर्की शासकों के आगमन पर अशराफ तबके की भाषा फ़ारसी को दरबार की भाषा का पद हासिल हुआ।फ़ारसी भाषा से भारतीय जनता अनभिज्ञ थी और भाषा की खाई ने इन दो वर्गों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया। पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली अपनी किताब ‘इतिहास का मतांतर’ में लिखते हैं – ‘जब तुर्कों के पतन के बाद ख़िलजी, तुग़लक़, लोधी सत्ता में आए तो फ़ारसी के वर्चस्व को आघात लगा क्यूँकि इन अफ़ग़ान शासकों की मातृभाषा फ़ारसी नही थी। इसके अलावा वे ईरान अद मध्य एशिया के उन अभिजात्य वर्ग के प्रति अपनी नफ़रत का प्रदर्शन करना चाहते थे, जिनकी भाषा फ़ारसी थी। जब मुग़ल को हराकर सूरी ‘यों’ ने सत्ता प्राप्त की तो उन्होंने भी खुले रूप में फ़ारसी के प्रति घृणा व्यक्त की। परंतु मुग़लों की दुबारा जीत ने फ़ारसी तथा विदेशी संस्कृति को नवजीवन प्रदान किया ।…जिन्होंने हमेशा अपने आप को भारत से तथा भारत की संस्कृति से खुद को अलग थलग रखा।… मुग़ल दरबार की आर्थिक तंगी के कारण ईरान से लेखकों कवियों का आना भी मंद पड़ गया तथा इस प्रकार फ़ारसी भाषा को भारत में जो ऊर्जा मिलती थी वह भी बुरी तरह प्रभावित हुई।’
ऐसे में जो वर्ग उर्दू को निम्न श्रेणी की भाषा मानता था और इसे सचेतन वर्ग की भाषा मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार न था, उस वर्ग ने उर्दू की शुद्धता के लिए कदम उठाए ताकि शासक और शासित श्रेणी की भाषा का अंतर स्पष्ट होकर उभरे। सिराजुद्दीन खान आरजू ने इस प्रक्रिया को तेज किया और उर्दू के स्तर को ऊँचा उठाया। उन्होंने इस तरह घोषणा की कि भाषा का स्तर अब संभ्रांत वर्ग के बोलने के काबिल हो गया है। पाकिस्तानी इतिहासकार मुबारक अली उर्दू के इस पक्ष पर मुहम्मद हुसैन आजाद की किताब ‘आबे हयात’ का उद्धरण देते हैं जिसमे मुहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं ‘ किस प्रकार से अरबी-फ़ारसीकरण ने उर्दू की जड़ें इसके अपने ही वातावरण से काट दी। भारतीय पृष्ठभूमि की सारी उपमा को दरकिनार कर उनके स्थान पर अरबी व फ़ारसी उपमाओं को भाषा पर थोप दिया गया। फलस्वरूप जो नए मुहावरे उभरे उनका ना तो भारत के सांस्कृतिक परिवेश से कोई सम्बंध था ना यहाँ के विचार से।’(1) यही से जन्म होता है ज़बान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला का जिसका शाब्दिक अर्थ है “उच्च उर्दू भाषा”। यह शब्द विशेष रूप से उर्दू भाषा के उस रूप को संदर्भित करता है जो साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, और जिसमें फारसी और अरबी शब्दावली का व्यापक उपयोग होता है। इस शब्द का उपयोग उर्दू के उस रूप के लिए किया जाता है जो मुगल दरबारों में विकसित हुआ और जो उच्च वर्ग और विद्वानों के बीच प्रचलित था। उर्दू-ए-मुअल्ला का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ, जब इसे शाही दरबारों में एक प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया गया। यह भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती थी और इसमें फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं के शब्द शामिल थे। इस प्रकार, उर्दू-ए-मुअल्ला को एक उच्च सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा के रूप में देखा गया, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में मुस्लिम पहचान का प्रतीक बन गई।
उर्दू: एक मुस्लिम पहचान
उर्दू की पहचान को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो राजनीति होती है, वह दोनों देशों की सांस्कृतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण को दर्शाती है। भारत में, उर्दू को अक्सर एक मुस्लिम भाषा के रूप में देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसे एक राष्ट्रीय और इस्लामी पहचान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विभाजन न केवल भाषाई बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।उर्दू का सांप्रदायिकरण मुख्यतः ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जब भाषा को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, उर्दू और हिंदी के बीच विवाद उभरा, जिसे हिंदी-उर्दू विवाद के रूप में जाना जाता है। इस विवाद ने भाषाई पहचान को धार्मिक पहचान के साथ जोड़ दिया। उर्दू को मुस्लिम समुदाय के साथ और हिंदी को हिंदू समुदाय के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इस प्रक्रिया में उर्दू को फारसी और अरबी शब्दावली के साथ अधिक जोड़ा गया, जिससे यह मुस्लिम सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गई। इस प्रक्रिया में पसमांदा जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज किया गया।
मुस्लिम लीग ने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। यह भाषा मुस्लिम समुदाय की एकता और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने के लिए चुनी गई थी।उर्दू को पाकिस्तान आंदोलन के दौरान एक एकीकृत भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले मुसलमानों को एकजुट कर सके। यह भाषा इस विचार का प्रतीक बनी कि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है जहां उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित किया जा सके। ब्रिटिश शासन के दौरान, उर्दू को प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में प्राथमिकता दी गई, विशेष रूप से उत्तर भारत में। यह निर्णय फारसी की जगह उर्दू को अपनाने के कारण लिया गया, जो कि मुस्लिम शासकों की भाषा थी। इससे उर्दू को मुस्लिम पहचान के साथ जोड़ा गया, जबकि हिंदी को हिंदू पहचान के साथ देखा जाने लगा। ब्रिटिश प्रशासन ने जनगणना और सांख्यिकी के माध्यम से भाषाई पहचान को और मजबूत किया। जनगणना रिपोर्ट्स में भाषाओं को धार्मिक समुदायों के साथ जोड़कर देखा गया, जिससे उर्दू को मुस्लिम और हिंदी को हिंदू समुदाय की भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसने भाषाई विभाजन को और गहरा किया और सांप्रदायिक पहचान को मजबूत किया।ब्रिटिश प्रशासन ने शिक्षा प्रणाली में भी उर्दू को बढ़ावा दिया, जिससे यह मुस्लिम समुदाय के बीच एक प्रमुख भाषा बन गई। यह प्रयास इस विचार को मजबूत करने के लिए था कि उर्दू न केवल एक सांस्कृतिक बल्कि एक प्रशासनिक भाषा भी है। उर्दू को हिंदी के विपरीत प्रस्तुत किया गया, जो हिंदू समुदाय के साथ अधिक जुड़ी हुई थी। इस प्रकार, उर्दू और हिंदी के बीच का विभाजन भी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के विभाजन को दर्शाने लगा।
उर्दू अदब के पसमांदा सवाल
यहां तक समझने के बाद आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि उर्दू का जन्म भले ही भारत के निम्न वर्ग में हुआ था लेकिन बाद में उर्दू अशराफों की ज़ुबान बनके रह गई। फ़ारसीकरण ने उर्दू को अशराफ मुस्लिम सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया।कहा जाता है कि किसी भी सभ्यता को मारना है तो उनकी भाषा को मार दो, सभ्यता अपने आप कब्र की पनाह ले लेती है। पसमांदा समूहों के लिए, भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब उनकी भाषा को दबाया या नष्ट किया जाता है, तो उनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ जाती है । पसमांदा समाज अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलता था पर अशराफ वर्ग पसमांदा समाज को अहल-ए-जबान में शामिल नहीं करते थे। इसका असर भी उर्दू अदब में नज़र आता है। 85% पसमांदा समाज को, उनकी समस्याओं को और उनकी संस्कृति को सिरे से ख़ारिज कर दिया गया है। जब किसी समुदाय की भाषा को दबाया जाता है, तो उनकी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। यह उन्हें सत्ता के ढांचे में और भी अधिक हाशिए पर धकेल देता है।
उर्दू अदब में प्रगतिशील आंदोलन का भी एक दौर चला है पर उनकी सारी प्रगतिशीलता अपनी जाति पर आकर खत्म हो गई। इन्होंने ख़ुदा की ज़ात को तो आड़े हाथों लिया पर अपनी जात पर कुछ नहीं लिखा।यह बताना न होगा कि प्रगतिशील आंदोलन के शुरुआती दौर में लिखने वाले सभी लोग उच्च जाति के थे। ये लेखक और शायर जाति का प्रयोग बस वहीं तक करते हैं जहाँ से ये अपने वर्ग-संघर्ष की बात शुरू कर सकें। उर्दू में ‘दलित मुसलमानों का अदब’ कहाँ है? इस विषय पर डॉक्टर अयूब राईन अपनी किताब ‘दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक’ में लिखते हैं कि ‘मुस्लिम वर्ग के लोग (अशराफ) अपनी कमी, कुरीतियों और सामाजिक नाइंसाफियों के बारे में खुद भी कम लिखता-बोलता हैं और दूसरे समाज के लोग यदि किसी भाषा-साहित्य के माध्यम से उन मुद्दों को उठाता है तो मुसलमानों के विशेष वर्ग (अशराफों) की तरफ से हंगामा खड़ा किया जाता है। ऐसी सूरत में उर्दू भाषा समेत अन्य भाषाओं पर पूरे मुस्लिम समाज अथवा पसमांदा अथवा दलित मुसलमानों के सम्बन्ध में लेखक प्राय: बचने की ही कोशिश करते रहते हैं।
उर्दू की तरक़्क़ी पसंद तहरीक और पसमांदा मुसलमान
चूंकि उर्दू पर अशराफ लोगों का वर्चस्व है इन्ही के पास तमाम संसाधन हैं। इसीलिए यही तय करते हैं कि ग़ज़ल के मौज़ूअ (मुद्दे) क्या हों! अगर पसमाँदा शायर और लेखक कुछ लिखते हैं तो उसे अदब के स्तर का ना मानकर ख़ारिज कर दिया जाता है। जब पसमांदा लेखकों को उनकी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के कारण अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह व्यक्ति ही सिर्फ ख़ारिज नहीं होता बल्कि उस भाषा में मौजूद साहित्य, कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। इससे पसमांदा समूहों की संस्कृति का ह्रास होता है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर खो जाती है।
पसमांदा शायर अदब में स्वीकार किए जाने की लालच में आज अपने लूम, साड़ी, कपड़े, बानी,खेती-किसानी, अपने मवेशी, कपड़े और अपने समाज की परेशानी वगैरह पर शेर न लिख कर अशराफ़ों की तरह औरतों की कमर उनकी ज़ुल्फों पर शायरी करता नज़र आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उर्दू अदब जाति ,से अंजान था। मिर्ज़ा हादी ‘रुस्वा’ की उमराव जान ‘अदा’ को ही लें। इस कहानी में नवाब छ्ब्बन साहब का एक दोस्त था ‘हुस्नु’ जो छब्बन साहब से बेईमानी करता है पर छ्ब्बन साहब की तवाएफ़ (किताब में रंडी लफ़्ज़ लिखा है) बिस्मिल्लाह को पता चल जाता है। इस पर बिस्मिल्लाह नवाब साहब से कहती है..
.बिस्मिल्लाह :- कहो तो नवाब हुस्नु को कोतवाली भिजवा दूँ?
नवाब (छ्ब्बन) :- नहीं, मेरे सर की क़सम! ऐसा न करना, सैयद है।
बिस्मिल्लाह :- सैयद काहे का! उस के बाप का तो पता नहीं।
नवाब :- ख़ैर वह तो अपने मुँह से कहता है।
उर्दू बचाव का नारा और पसमांदा
ब्रिटिश राज में ही ये तय हो गया था कि अंग्रेज़ी वो जबान है जिसके दम पर आप ऊंचे ओहदे को हासिल कर सकते हो। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने जहाँ एक ओर अशराफ तबके के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई पर जोर डाला वहीं दूसरी और पसमांदा समाज में आधुनिक शिक्षा की खिलाफत करते रहे।(2) यह भी दिलचस्प है कि अंग्रेज़ी पढे लिखा यह वर्ग उर्दू बचाव के नाम पर भारत विभाजन का भी पक्षधर बन गया और पसमांदा मुसलमानों को यह समझाने लगा कि भारत का विभाजन नहीं हुआ तो उर्दू नहीं बचेगी। मौजूदा दौर में उर्दू और मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे के पर्याय की तरह देखे जाते हैं। नतीजतन पसमांदा मुसलमानों पर उर्दू बचाने का दबाव है पर अशराफ के लड़के तो अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं तो ऐसे में उर्दू बचाने की जिम्मेदारी पसमांदा के कंधों पर आ गई लेकिन उर्दू पढ़े-लिखे पसमांदा लिए नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। जरा यह आंकड़े देखें जिसे प्रोफेसर मसऊद आलम फलाही जी ने अपनी किताब ‘हिंदुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान'(Al-Qazi Publication, New Delhi, 2020) में दिया है- इंजीनियर शमी खान खटाना और आयशा समन साहिबा ने
भारत की 21 यूनिवर्सिटी में मुसलमानों से संबंधित विभागों जैसे उर्दू ,अरबी, पारसी, फारसी, इस्लामिक स्टडी इत्यादि में शिक्षकों (असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर) की सामाजिक स्थिति पर जानकारी एकत्र की जिसके अनुसार – कुल 296 शिक्षकों में कथित अशराफ वर्ग के शिक्षक 272 हैं, अनुसूचित जाति के 3 शिक्षक, अनुसूचित जनजाति के 3 शिक्षक, अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 शिक्षक हैं। मतलब करीब 92% अशराफ शिक्षक हैं और ये साफ है कि शिक्षा से जुड़े हर संसाधन पर इन्ही की नुमाइंदगी चलती होगी। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू बचाने की ज़िम्मेदारी पसमांदा की है और उर्दू से कमाने की और अपना सत्ता वर्चस्व बनाए रखने की ज़िम्मेदारी अशराफों की है।
उर्दू अदब में पसमांदा औरतें
उर्दू अदब में एक अशराफ़ लेखक के लिए 3 प्रकार की औरतें उसकी ज़िन्दगी में आती हैं, पहली तवायफ़, दूसरी नौकरानी और तीसरी उसकी बीवी। हम यह देखते हैं कि तवायफ़ और अपनी बीवी यानी अपने घर की संस्कृति और अपने वर्ग की चेतना पर तो इन लोगों ने ख़ूब लिखा है पर बात जब नौकरानियों की होती है तो इनकी क़लम शांत हो जाती है। यहाँ इस बात को समझें कि भारत के इतिहास में वर्ग और जाति तक़रीबन एक जैसी ही रही हैं। जब हम नौकर या नौकरानियों की बात करते हैं तो दरअसल हम उस वक़्त पसमांदा समाज की बात कर रहे होते हैं। पसमांदा महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और उनके पास शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हैं। उर्दू साहित्य में इस वर्ग की महिलाओं को अक्सर घरेलू कामकाज में संलग्न दिखाया जाता है, और उनके संघर्षों को मुख्यधारा के साहित्य में कम ही जगह मिलती है। अगर इतिहास के आईने में हमें अपनी अपमानित छवि नज़र नही आती तो हम बौद्धिक अपंग हो चुके हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास ‘कुठाँव’ में दलित मुस्लिम लड़की ‘हुमा’ का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है :- जिसका चेहरा चौड़ा था. आँखें फैली-फैली सी थीं। होंठ बर्फी के तराशे हुए टुकड़ों की तरह। छातियों पर अमरुद जैसी कुछ आकृतियां उभरी हुई थी। नाक ऐसी जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो मतलब कि ऐसी शक्ल सूरत की लड़कियां बदसूरत होती हैं। ये सोच पुरे तरीके से रंग भेदी है जहाँ गोरी नस्ल की जिस्मानी खासियतों को सुंदरता का मापदंड माना जाता है। हमारी सुंदरता की समझ अशराफिया ही क्यों है? खां साहब के घर की लड़की ‘ज़ुबैदा’ तथकथित खूबसूरत लड़की है. अरे सितारा भी तो खूबसूरत ही है पर वह तो हलालखोर यानि हेला है. खा गए न धोखा दलित लड़की खूबसूरत कैसे हो सकती है? क्या सितारा का बाप एक अशराफ था…? डॉक्टर अयूब राईन अपनी किताब ‘दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक’ में लिखते हैं कि उर्दू ग़ज़ल को महबूब से बातें करना कहा गया है। यह महज़ इत्तेफ़ाक़ नहीं है कि उर्दू ग़ज़लों में महबूबायें चांद जैसी गोरी हुआ करती हैं। क्या उर्दू शायरी में ऐसी किसी महबूबा को सामने रखा गया है, जो दलित मुस्लिम समाज से हो? क्योंकि वह तो चाँद जैसी गोरी नहीं होती? यह रंगभेद उर्दू ग़ज़लों की शान है। अयूब राईन आगे लिखते हैं कि महिला हितों की बात उठाने वाली अशराफ लेखिका अपनी कहानी ‘दो हाथ’ में बहुसंख्यक हलालखोर समाज की चर्चा करती हैं पर उन्हें मुंबई महानगर (जहाँ वह रहती थी) में स्थित हज हाउस के पैखानों को साफ़ करने वाली महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखा?
जिस प्रकार ‘पंचतंत्र’ की कहानियों में जानवर मुख्य पात्र होते हुए भी वे वास्तविकता में इंसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कहानियाँ इंसानों के बारे में हैं, जिनमें जानवर केवल प्रतीक (signifier) हैं, जबकि उनके पीछे का अर्थ (signified) इंसान होते हैं। इसी तरह, सवर्ण लेखकों ने दलित पात्र तो खड़े किए, लेकिन वे केवल प्रतीकात्मक रूप से दलित थे; असल में वे सवर्ण मानसिकता को ही दर्शाते थे। Saussure ने भाषा को signifier और signified के मेल के रूप में समझाया, जैसे प्रेमचंद की ‘कफ़न’ कहानी के दलित पात्र बाहरी रूप से दलित दिखते हैं, पर असल में उनका चरित्र सवर्ण है।उदाहरण के लिए, “कफ़न” कहानी में घीसू और माधव का चरित्र दलित होते हुए भी उच्च जाति की सोच को दर्शाता है। प्रेमचंद ‘ईदगाह’ कहानी लिखते हैं पर उस बूढ़ी औरत की जाति नहीं बताते और जो पसमांदा जाति पर कुछ लिखते हैं जैसे गुलज़ार की कविता “यार जुलाहे” तो वह अपनी कविता में जुलाहों की समस्याओं को अनदेखा कर उनके पेशे को रोमांटिक बना देते हैं। इस तरह की रोमांटिसाइज़ेशन से समस्याओं को केवल बेचा जाता है, अपनाया नहीं जाता।
हर भाषा के अस्तित्व का अपना महत्त्व है, क्योंकि भाषा में मानव जाति का अस्तित्व समाहित है। जैसे-जैसे हमारे फ़लसफे वक्त के साथ बदलते हैं वैसे-वैसे हमारी जुबान में भी बदलाव झलकने लगता है। उर्दू को पसमांदा समुदाय के दर्शन और आत्मा से कौन मिलवाएगा? यह काम अशराफ़ समुदाय से उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि वर्तमान उर्दू साहित्य पर उनका प्रभुत्व है, और यह साहित्य उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों से प्रभावित है। पसमांदा समुदाय को अपने दर्द और संघर्षों को अपनी भाषा में व्यक्त करने की आवश्यकता है। पसमांदा समुदाय को अपनी लड़ाई को आवाज़ देने के लिए अपनी भाषा को गढ़ना और मजबूत करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि वे अपने इतिहास में हुई हर नाइंसाफी और उसके प्रतिरोध को दर्ज करें। यह केवल साहित्यिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो पसमांदा समुदाय की आवाज़ को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करेगा। सबसे ज़रूरी यह है कि मौजूदा उर्दू अदब, जो कि अशराफ जातियों का अदब है, उसे रद्द करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे पूरी तरह से नकार दिया जाए, बल्कि इसकी आलोचना करते हुए इसे पुनः परिभाषित किया जाए ताकि यह सभी समुदायों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को समाहित कर सके। इस प्रकार, भाषा के माध्यम से पसमांदा समुदाय की आवाज़ को सशक्त बनाना और उनके अनुभवों को साहित्य में स्थान देना, एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में अग्रसर करेगा।
उर्दू ज़ुबान का पसमांदा अदब, अशराफ अदब की कब्र पर उगेगा:-
सुनो अशराफ़!
मैं तुम्हारी संस्कृति को रद्द करता हूँ
तुम्हारी उन सभी रिवायतों को रद्द करता हूँ
जो जन्म आधारित श्रेष्ठता की वकालत करती हैं
मैं तुम्हारे उस अदब को भी रद्द करता हूँ
जिस में पसमांदा समाज का दर्द नज़र नहीं आता
सुनो! हम ने तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह का शंख फूक दिया है
नहीं स्वीकार करते हम, इस्लाम की तुम्हारी व्याख्या को
जहाँ एक सैयद और एक हलालखोर में भेद है।
हम ने अपना उद्देश्य पा लिया है,
जाहिलियत की सभी रस्में आज से खत्म हुईं
तरजीह और बरतरी के सभी दावे,
खानदान, माल-ओ-दौलत के सभी दावे
जिसे अपने पैरों के नीचे रौद दिए थे मेरे नबी (स०अ०व०) ने
सुनो! आज हम भी रौंदते हैं
सय्यदों की श्रेष्ठता के सभी दावों को
नबी (स०अ०व०) की आल बन कर।
~ अब्दुल्लाह मंसूर

संदर्भ :
1- मुबारक अली, इतिहास का मतान्तर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण २००२, पेज:117-118
2-सर सय्यद अहमद खां : व्याख्यान एवं भाषणों का संग्रह, संकलन : मुंशी सिराजुद्दीन, प्रकाशन : सिढौर 1892, ससंदर्भ अतीक़ सिद्दीक़ी : सर सय्यद अहमद खां एक सियासी मुताला, अध्याय : 8, तालीमी तहरीक और उस की मुखालिफ़त, शीर्षक : गुरबा को अंग्रेज़ी तालीम देने का खयाल बड़ी ग़लती है, पृष्ठ : 144/145
https://www.newageislam.com/books-and-documents/caste-and-caste-based-discrimination-among-indian-muslims—part-12–modern-indian-ulema-on-the-caste-question/d/3678
3:- डॉ. अयुब राईन, दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक, शशि प्रकाशन, बिहार, सुपौल, पहला संस्करण,2022
4:- मसऊद आलम फ़लाही, हिन्दुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान, आइडियल फाउंडेशन, मुम्बई, संस्करण २००९ पेज 581
लेखक, पसमांदा एक्विस्ट तथा पेशे से शिक्षक हैं। Youtube चैनल Pasmanda DEMOcracy के संचालक भी हैं।