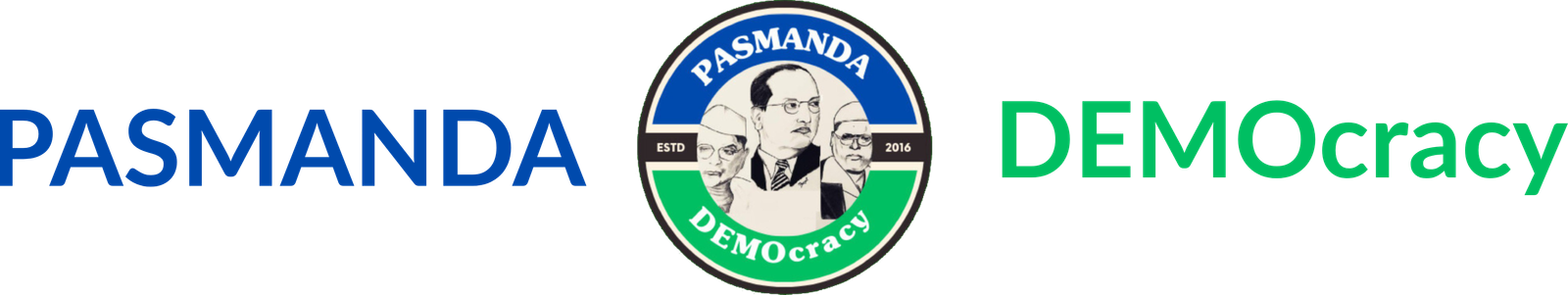~ डॉ. उज़्मा खातून
2019 में घोषित मक्का चार्टर, कोई नई खोज या इस्लाम को बदलने की कोई आधुनिक कोशिश नहीं है। सच तो यह है कि यह उस आस्था के असली पैगाम की ओर एक ज़बरदस्त वापसी है— एक ऐसा पैगाम जो शांति, बराबरी और साथ मिलकर रहने का था, और जिसकी शुरुआत पैगंबर मुहम्मद के समय में हुई थी। आधुनिक मक्का चार्टर की सच्ची भावना और गहरे अर्थ को समझने के लिए, हमें पहले मदीना शहर में पैगंबर के अपने बुनियादी उदाहरण को देखना होगा।
जब पैगंबर मुहम्मद 622 ईस्वी में मदीना आए, तो वह एक ऐसे शहर में पहुँचे जो बुरी तरह से बँटा हुआ था। दशकों से, अलग-अलग कबीले आपस में लड़ रहे थे, और लोग सिर्फ अपने गुट के वफादार थे। दो मुख्य अरब कबीले, अवस और खज़रज, एक कड़वे झगड़े में फँसे थे। ताकत से कब्ज़ा करने के बजाय, पैगंबर ने एक बहुत ही असाधारण और दूरदर्शी राजनीतिक कदम उठाया। उन्होंने एक लिखित संविधान बनाया, जिसे आज हम ‘मदीना का संविधान’ (Constitution of Medina) के नाम से जानते हैं।
इस ऐतिहासिक दस्तावेज़ ने मुसलमानों, यहूदियों और अन्य कबीलों को एक साथ लाकर एक एकजुट समुदाय— ‘उम्मा’ (Ummah)— बनाया। इसकी पहली ही पंक्ति, “हम एक समुदाय हैं,” ने एक नए तरह के समाज की नींव रखी। यह एक ऐसा समाज था जो तंग कबीलाई या धार्मिक पहचान पर नहीं, बल्कि सबकी सुरक्षा और भलाई के लिए ‘साझी नागरिकता’ और ‘सामूहिक ज़िम्मेदारी’ के क्रांतिकारी विचारों पर बना था। मदीना का यह बुनियादी संविधान ही वह असली मिसाल था, जिसके मूल उसूलों को आधुनिक मक्का चार्टर पूरी दुनिया के लिए वापस लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
“उम्मा” शब्द का इस्तेमाल कुरान में कई बार हुआ है। यह साझा विश्वासों से जुड़े एक एकजुट समुदाय को दिखाता है। शुरू में, इसका मतलब एक पैगंबर के नेतृत्व वाला समूह था, लेकिन बाद में यह विचार इस्लाम के सभी मानने वालों तक फैल गया। सदियों में यह धर्म दुनिया भर में फैला, ‘उम्मा’ का नेतृत्व खलीफाओं ने किया, जिन्होंने बड़े इस्लामी समुदाय के भीतर सरकार और प्रशासन को व्यवस्थित किया।
पैगंबर मुहम्मद ने अपनी शिक्षाओं से शुरुआती मुसलमानों को एकजुट कर इस पहले ‘उम्मा’ की ज़मीन तैयार की, लेकिन यह मदीना का संविधान था जिसने इस एकता को राजनीतिक तौर पर पक्का किया। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि आस्था का बंधन पुराने पारिवारिक या कबीलाई रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी है। इसने विशेष रूप से यहूदी कबीलों का समुदाय में बराबर के सदस्यों के तौर पर स्वागत किया, जिनके अधिकार और आज़ादी सुरक्षित थे।
सबको शामिल करने का यह एक मुख्य सिद्धांत था; इस नए राजनीतिक ‘उम्मा’ का सदस्य होना सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं था। यह हर उस इंसान के लिए था जिसने पैगंबर के नेतृत्व को स्वीकार किया और चार्टर की शर्तों को माना। इस शुरुआती विविधता, जिसमें अलग-अलग नस्ल और समाज के लोग शामिल थे, को इस्लाम के साझा नैतिक सिद्धांतों पर आधारित भाईचारे के एक तंत्र के ज़रिए बढ़ावा दिया गया। यह इस्लाम से पहले की ‘असबीय्या’ (कबीलाई एकजुटता) की सोच से एक बड़ा बदलाव था, जहाँ वफादारी सिर्फ अपने कबीले के लिए होती थी, जो अक्सर बदला और लड़ाई-झगड़े के न खत्म होने वाले चक्र को जन्म देती थी।
मदीना चार्टर के सिद्धांत सचमुच अपने समय से बहुत आगे थे। धार्मिक आज़ादी को साफ तौर पर सुरक्षित किया गया था। दस्तावेज़ ने यहूदियों और अन्य गैर-मुस्लिम कबीलों को अपने धर्म को मानने और अपनी परंपराओं के मुताबिक इबादत करने के पूरे अधिकार को मान्यता दी, बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती या परेशानी के
धार्मिक आज़ादी की इस घोषणा ने आस्था को एक निजी पसंद का मामला बना दिया, न कि कुछ ऐसा जिसे राज-सत्ता काबू करे। इन अधिकारों के साथ, चार्टर ने स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ भी तय कीं। इसने एक ‘सामूहिक सुरक्षा समझौता’ बनाया, जिसमें सभी समुदायों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, यह ज़रूरी था कि अगर शहर पर बाहर से हमला हो तो वे एक-दूसरे की रक्षा करें।
न्याय और कानून के राज को हर किसी के लिए एक कर्तव्य माना गया। यह पक्का किया गया कि झगड़ों का निपटारा तय किए गए सिद्धांतों के आधार पर हो, न कि कबीलाई पक्षपात या ताकत के मनमाने इस्तेमाल पर। जैसा कि जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के एक सम्मानित प्रोफेसर डॉ. जॉन एल. एस्पोसिटो ने कहा है: “मदीना चार्टर इतिहास का शायद पहला लिखित संविधान हो सकता है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी देता है। यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसे यूरोप को खोजने में सदियाँ लग गईं।” इसलिए, पैगंबर न सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी थे, जिन्होंने कई धर्मों वाले समाज के लिए कानून बनाए, जिससे ‘सह-अस्तित्व’ (एक साथ रहना) समुदाय का एक आधिकारिक और सुरक्षित हिस्सा बन गया।
हालाँकि, असली ‘उम्मा’ की इस एकजुट और सबको शामिल करने वाली सोच को सदियों से भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक असर की वजह से। यूरोपीय साम्राज्यों ने एक ऐसा दौर शुरू किया जिसने मुस्लिम दुनिया को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसकी शुरुआत भारत में ब्रिटिश जीत और बाद में अफ्रीका पर कब्ज़े की होड़ से हुई।
पहले विश्व युद्ध के बाद, अरब ज़मीनों पर कब्ज़े और ‘साइक्स-पिकॉट समझौते’ ने इस इलाके का नक्शा ही बदल दिया। इसे बनावटी ‘राष्ट्र-राज्यों’ (nation-states) की लकीरों पर बाँट दिया गया, जिसने गहरी नस्ली दरारें पैदा कीं और एकता की किसी भी कोशिश को रोक दिया। शाही ताकतों ने इन दरारों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और सांस्कृतिक, भाषाई या धार्मिक रिश्तों की परवाह किए बिना सरहदें खींच दीं। इन औपनिवेशिक विरासतों, जिन्हें अक्सर आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलनों ने भी जारी रखा, ने उस फूट, विदेशी-विरोध और नस्लवाद को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है, जो ‘उम्मा’ की असली भावना को कमज़ोर करते हैं।

इसी टूटी हुई आधुनिक सच्चाई के जवाब में मक्का चार्टर का गहरा महत्व समझ आता है। मई 2019 में, रमज़ान के पवित्र महीने में, एक दुर्लभ और ऐतिहासिक समझौता हुआ। 139 देशों के 1,200 से ज़्यादा मुस्लिम विद्वान और नेता, जो 27 अलग-अलग फिरकों और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे थे, मक्का में इकट्ठा हुए। इस सम्मेलन की मेज़बानी ‘मुस्लिम वर्ल्ड लीग’ ने की और इसकी अध्यक्षता डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल-इस्सा ने की। उनका मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि गहरा नैतिक था: इस्लाम की सच्ची, दयालु भावना को उन अतिवादियों से वापस लेना जो इसके पैगाम को तोड़-मरोड़ रहे हैं, और उन ‘इस्लामोफोब’ (इस्लाम से नफरत करने वालों) से (बचाना) जो इस पर हमला करते हैं।
इसका नतीजा 30-बिंदुओं वाला “मक्का चार्टर” था, जो आधुनिक युग के लिए पाँच बड़े सुधारों को साफ तौर पर लिखता है। यह मुस्लिम-बहुल देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने, बँटवारे, नस्लवाद और नफरत फैलाने वाली बातों (hate speech) की निंदा करने, गैर-मुस्लिमों के लिए बराबर की नागरिकता स्थापित करने, महिलाओं और युवाओं को नेतृत्व में ज़्यादा ताकतवर बनाने, और जंगी फतवों और धर्म के राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल को सख्ती से खारिज करने की अपील करता है।
यह आधुनिक चार्टर अपनी ताकत और अधिकार उन्हीं स्रोतों से लेता है, जिनसे इसके ऐतिहासिक पुरखे (मदीना चार्टर) ने लिया था: कुरान, पैगंबर का उदाहरण, और विद्वानों की आम सहमति, यानी ‘इज्मा’। पुराने इस्लामी सोच में, जब विद्वानों का इतना बड़ा और विविध समूह किसी बात पर सहमत हो जाता है, तो वह आम सहमति मुख्यधारा की मान्यता का एक आधिकारिक बयान बन जाती है।
इस वैश्विक सहमति ने चार्टर को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है, और यह एक मज़बूत पैगाम देती है कि सहनशीलता, सह-अस्तित्व (मिल-जुलकर रहना), और शांति ही इस्लाम की सच्ची नींव हैं। मक्का में जो एकता दिखी— जहाँ सुन्नी, शिया, सूफी और दूसरे समूह एक साथ खड़े थे — वह खुद एक जीती-जागती मिसाल थी कि इस्लाम का मुख्य पैगाम सांप्रदायिक बँटवारे से कहीं बड़ा है।
जैसा कि डॉ. अल-इस्सा ने ज़ोरदार तरीके से कहा, “मक्का चार्टर हमारे समय के लिए वही है जो मदीना चार्टर पैगंबर के समय के लिए था… मिल-जुलकर रहने के लिए एक नैतिक संविधान।” यह चार्टर “सभ्यतागत साझेदारी,”(civilizational partnership) “व्यापक नागरिकता,”(comprehensive citizenship) और “जोड़ने वाली साझी चीज़ों”(the uniting commonalties) जैसे नए और गहरे विचार पेश करता है। ये विचार मानवाधिकारों की वैश्विक समझ को और पक्का करते हैं और अतिवाद और नफरत से दूर एक रास्ता दिखाते हैं। चार्टर का आधुनिक विषयों जैसे महिलाओं को सशक्त बनाना, नागरिकता को विस्तार देना, पर्यावरण की रक्षा करना, और मुस्लिम युवाओं की पहचान को मज़बूत करने पर ध्यान देना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यह बुनियादी सिद्धांतों पर ज़ोर देता है जैसे सभी इंसानों की एक ही उत्पत्ति, नस्लवाद और खुद को बड़ा समझने के दावों को खारिज करना, और सांस्कृतिक व धार्मिक विविधता को ईश्वर की एक योजना के तौर पर स्वीकार करना।
यह चार्टर अतिवाद के खिलाफ एक सीधा धार्मिक तर्क पेश करता है। यह ‘तकफीर’ (takfir) को साफ तौर पर खारिज करता है — यानी दूसरे मुसलमानों को काफिर (धर्म से बाहर) घोषित करने की खतरनाक प्रथा, जिसे हिंसक गुटों ने हत्या को जायज़ ठहराने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बजाय, यह सभी इस्लामी परंपराओं के बीच भाईचारे की अपील करता है। यह एक ‘बिना-सरहद वाली खिलाफत’ की हिंसक विचारधारा को खारिज करता है, और आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की वैधता की पुष्टि करता है और मुसलमानों को अपने देशों का वफादार, कानून-पसंद नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इसके अलावा, यह विविधता को ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा मानकर उसका स्वागत करता है, यह सिखाता है कि धर्म और संस्कृति में अंतर ज्ञान की निशानियाँ हैं, न कि झगड़े की वजह। सहनशीलता को मज़बूती से आस्था में पिरोकर, यह चार्टर मुसलमानों को दूसरों के साथ शांति से रहने के लिए एक मज़बूत धार्मिक कारण देता है।
सोशल मीडिया के युग में, जहाँ कम-जानकारी वाले इंफ्लुएंसर (influencers) अक्सर इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करते हैं, यह दस्तावेज़ असली विद्वानों के अधिकार को भी बहाल करता है, और समुदाय को याद दिलाता है कि वे उन लोगों से मार्गदर्शन लें जिनके पास गहरा ज्ञान और नैतिक ईमानदारी है।
यह चार्टर इस्लामी संस्कृति और सभ्यता की सच्ची तस्वीर को बढ़ावा देकर ‘इस्लामोफोबिया’ का मुकाबला करने के लिए एक योजना देता है, जो एक रक्षात्मक स्थिति से हटकर एक सक्रिय पहल की तरफ ले जाता है। इसे एक “ऐतिहासिक संविधान” कहा गया है जिसे अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों और फिरकों के लोगों के बीच मिल-जुलकर रहने के मूल्यों को स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक उम्मीद भरा दस्तावेज़ है जो नस्ली झगड़े और अतिवाद के खिलाफ खड़ा है। यह असली कदम उठाने की अपील करता है, जैसे नफरत फैलाने वालों को सज़ा देने के लिए कानून बनाना, आतंकवाद और अन्याय से लड़ना, महिलाओं को सशक्त बनाना, और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाना।
यह दस्तावेज़ इस्लाम की सदाबहार शिक्षाओं को आज की वैश्विक चुनौतियों से शानदार तरीके से जोड़ता है। पर्यावरण की रक्षा करने की इसकी अपील कुरान के उस विचार पर आधारित है कि इंसान धरती पर ईश्वर के ‘खलीफा’ (प्रतिनिधि) हैं, जो पर्यावरण की रक्षा को एक धार्मिक ज़िम्मेदारी बनाती है।
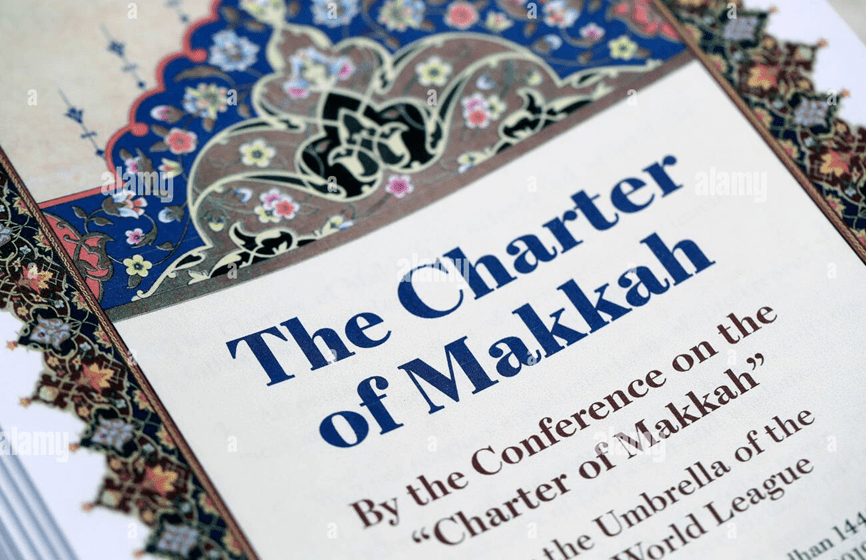
मानवाधिकारों, गरिमा, और बराबरी के लिए इसकी हिमायत (समर्थन) इस्लामी कानून (शरीयत) के ऊँचे मकसदों (Maqasid al-Shari‘ah) से पूरी तरह मेल खाती है, जिनका लक्ष्य धर्म, जीवन, बुद्धि, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना है। इस तरह, यह चार्टर सिर्फ पश्चिमी विचारों की नकल नहीं कर रहा है, बल्कि आधुनिक लोगों के लिए सच्चे इस्लामी विचारों को दोबारा हासिल कर रहा है और उन्हें फिर से पेश कर रहा है।
बेशक, चार्टर की कामयाबी आखिरकार इस पर ईमानदारी से अमल किए जाने पर निर्भर है। हालाँकि आलोचक राजनीतिक हितों के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन इसका नैतिक और धार्मिक मूल्य नकारा नहीं जा सकता। सबसे हौसला बढ़ाने वाला संकेत यह है कि इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल पहले ही शुरू हो चुका है। नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने इसके विचारों को अपने ‘अंतर-धार्मिक’ शांति कार्यक्रमों और स्कूली पाठ्यक्रम में अपनाना शुरू कर दिया है, जो आपसी सद्भाव बनाने की इसकी असली काबिलियत को दिखाता है।
इसके अलावा, इसे अफ्रीका में इमामों के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में, यूरोप में अलग-अलग इस्लामी फिरकों के बीच बातचीत में, और दुनिया भर में अलग-अलग धर्मों के मंचों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चार्टर को एक जीता-जागता दस्तावेज़ बनाने के लिए, शिक्षा को केंद्र में होना चाहिए। इसे धार्मिक स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि भविष्य के नेता इसके मूल्यों के साथ बड़े हों।
मुस्लिम संगठन इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल नफरत भरी बातों, असमानता, और पर्यावरण के विनाश के खिलाफ अभियानों में कर सकते हैं। युवाओं को अतिवाद से बचाने की इसकी अपील खास तौर पर ज़रूरी है, जिसमें ऐसे मंचों की कल्पना की गई है जहाँ नौजवान मुसलमान बातचीत में शामिल हो सकें और एक आत्मविश्वासी, दयालु इस्लामी पहचान बना सकें जो कट्टरपंथ के आकर्षण का मुकाबला कर सके।
मक्का चार्टर इस्लाम के असली वादे का एक नवीनीकरण है— यह उस इंसाफ-पसंद और सबको साथ लेकर चलने वाले समाज की एक ज़बरदस्त याद दिलाता है जिसे पैगंबर मुहम्मद ने चौदह सदियों पहले मदीना में बनाया था। यह मुसलमानों को उस रहमदिल (दयालु) और सहयोग करने वाले इस्लाम को फिर से खोजने का न्योता देता है जिसने कभी इंसानियत को साझा नैतिक मूल्यों के तहत एकजुट किया था।
इसकी सोच पर अमल करके, दुनिया भर का मुस्लिम समुदाय एक बार फिर दुनिया के लिए शांति और नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत बन सकता है। चार्टर का पैगाम साफ़ है: इस्लाम की सच्ची ताकत सत्ता में नहीं, बल्कि रहम में है; दबदबा कायम करने में नहीं, बल्कि इंसाफ में है; अलग-थलग रहने में नहीं, बल्कि सहयोग में है। यह आगे बढ़ने का एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो मुसलमानों को उनकी शानदार विरासत से दोबारा जोड़ता है और साथ ही उन्हें भरोसे के साथ शांति, सद्भाव और सार्वभौमिक इंसानी गरिमा के भविष्य की तरफ ले जाता है।
डॉ. उज़्मा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व फैकल्टी, एक लेखिका, स्तंभकार और सामाजिक विचारक हैं।
अनुवाद: अब्दुल्लाह मंसूर