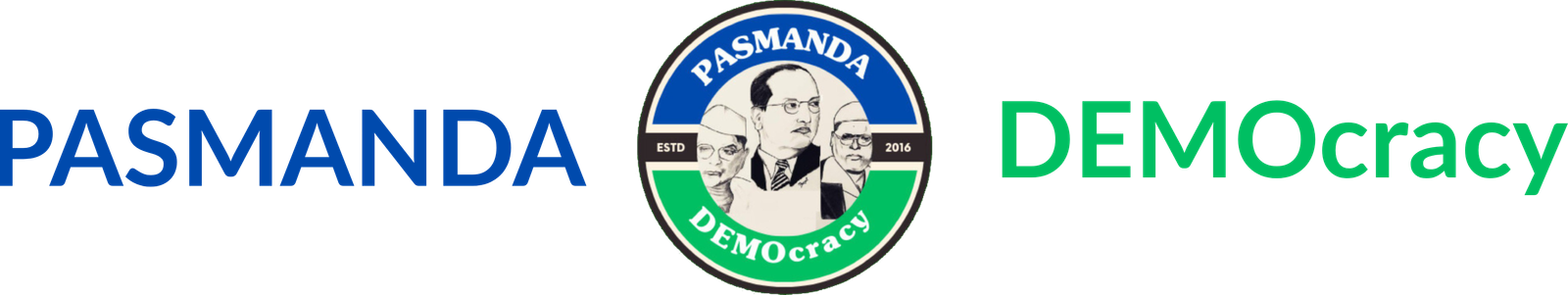डॉ. उज्मा खातून
कर्बला की जंग का अंत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं था, बल्कि इस्लामी इतिहास का एक गहरा, दर्दनाक और बदलाव लाने वाला नया दौर शुरू हुआ। जब पैग़ंबर मुहम्मद (स.अ.) के प्यारे नवासे इमाम हुसैन (र.अ.) 10 मुहर्रम को शहीद हुए, तो उनके साथ सिर्फ लोग नहीं मरे—बल्कि एक आंदोलन, एक सोच और एक रास्ता भी जन्मा, जिसने मुसलमानों को लंबे समय तक प्रभावित किया।
कर्बला के बाद शिया मुसलमानों ने खुद को बाकी मुस्लिम दुनिया से अलग महसूस किया। वे खुद को सच्चाई के लिए कष्ट सहने वाला समुदाय मानते थे। धीरे-धीरे, अली (र.अ.) के ख़ानदान के प्रति वफ़ादारी केवल राजनीति नहीं रही, बल्कि आस्था और पहचान का हिस्सा बन गई। शियाओं का यह मानना बन गया कि मुसलमानों की सही रहनुमाई सिर्फ अली के वंशजों, यानी इमामों के हाथ में होनी चाहिए।
कर्बला के बाद जो लोग बच गए—ज्यादातर औरतें और बच्चे—उन्हें क़ैद करके दमिश्क (सीरिया) ले जाया गया। उनके साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन (र.अ.) भी थे, जो बीमारी के कारण लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाए थे और इसलिए ज़िंदा बचे। इन क़ैदियों के ज़रिए ही कर्बला का पैग़ाम दुनिया तक पहुँचा। हुसैन (र.अ.) की बहन ज़ैनब (र.अ.) ने यज़ीद के दरबार में बहादुरी से भाषण दिया और दुनिया को याद दिलाया कि असली फ़तह उन लोगों की है जो इंसाफ़ के लिए शहीद हुए, न कि उन ज़ालिमों की जिन्होंने उन्हें मारा।
क़ैद से रिहा होकर अहल-ए-बैत (पैग़ंबर का घराना) के लोग मदीना लौटे, मगर अब दुनिया बदल चुकी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन (र.अ.) ने लड़ाई के बजाय इबादत, सब्र और दुआओं का रास्ता चुना। उन्होंने सहीफ़ा सज्जादिया नाम की दुआओं की किताब लिखी, जो आज भी बहुतों की रूहानी रहनुमाई करती है। उन्होंने तलवार से नहीं, बल्कि अपने अल्फ़ाज़ और इबादत से कर्बला के पैग़ाम को ज़िंदा रखा।
मगर सब चुप रहने के हामी नहीं थे। ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले भी थे। इमाम ज़ैद इब्न अली (र.अ.), जो ज़ैनुल आबिदीन (र.अ.) के बेटे थे, उन्होंने कई साल बाद बनी उमय्या के ख़िलाफ़ तलवार उठाई। लेकिन कूफ़ा के वही लोग जिन्होंने पहले वफ़ादारी का वादा किया था, उन्होंने धोखा दे दिया। इमाम ज़ैद भी शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी से शिया मज़हब की ज़ैदी शाखा की शुरुआत हुई। ज़ैदी मानते थे कि कोई भी नेक और बहादुर शख़्स जो अली (र.अ.) के वंश से हो, वह इमाम बन सकता है। उनके यहां इमामत खानदानी नहीं बल्कि पात्रता से तय होती थी। उस दौर में “बारह इमामों” का विचार अभी सामने नहीं आया था।
इमाम जाफ़र अल-सादिक़ (र.अ.) शिया इस्लाम के एक अहम रहनुमा बने। उन्होंने कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दीं और शिया अक़ीदे को एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्हीं के दौर में शिया और सुन्नी इस्लाम में सोच और धार्मिक ढांचे में फर्क और स्पष्ट हुआ। जाफ़र अल-सादिक़ (र.अ.) को सुन्नी और शिया दोनों इज्ज़त देते हैं। वह उस समय जिए जब उमय्या ख़िलाफ़त गिर रही थी और अब्बासी सत्ता बन रही थी।
इमाम जाफ़र (र.अ.) की मौत के बाद फिर मतभेद हुआ। कुछ लोगों ने उनके बेटे इस्माईल (र.अ.) को अगला इमाम माना और कहा कि वह छुप गए हैं। ये लोग इस्माइली कहलाए और बाद में फ़ातिमी ख़िलाफ़त बनाए जो मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और येरुशलम तक फैली। दूसरे लोगों ने मूसा अल-काज़िम (र.अ.) को इमाम माना, और ये “बारह इमामी शिया” कहलाए, जो मानते हैं कि बारह इमामों की एक पंक्ति है और आख़िरी इमाम—मुहम्मद अल-महदी (र.अ.)—ग़ायब हैं और एक दिन लौटेंगे। आज दुनिया के ज़्यादातर शिया “इमामिया” यानी बारह इमामी परंपरा से हैं।
इसी बीच एक और अहम आवाज़ उठी—अब्दुल्ला इब्न जुबैर (र.अ.) ने यज़ीद की हुकूमत को मानने से इनकार कर मक्का में खुद को ख़लीफ़ा घोषित किया। जब मदीना में यज़ीद की फौज ने हर्रा की लड़ाई में कत्लेआम किया और मक्का का घेराव किया तो काबा तक को नुकसान पहुँचा। यज़ीद की अचानक मौत के बाद हुकूमत में अफ़रातफ़री फैल गई।
बाद में मरवान इब्न हकम (र.अ.) और उनके बेटे अब्दुल मलिक (र.ह.) के ज़रिए बनी उमय्या ने दोबारा सत्ता संभाली। उनका जालिम जनरल हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का में अब्दुल्ला इब्न जुबैर (र.अ.) को क़त्ल किया। सुकून आया—लेकिन यह सुकून डर का था, इंसाफ़ का नहीं।
बनी उमय्या ने अरबी नस्ल वालों को तरजीह दी और गैर-अरबी मुसलमानों (मवाली) के साथ भेदभाव किया। एक अपवाद थे—उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (र.ह.), जिन्होंने कुछ सुधार लाने की कोशिश की, मगर उनकी हुकूमत थोड़े वक्त की थी।
उधर ख़ुरासान (आज का ईरान-उज्बेकिस्तान का इलाक़ा) में अब्बासियों ने अबू मुस्लिम अल-ख़ुरासानी (र.ह.) के ज़रिए एक बड़ी बगावत शुरू की। उनकी फौज काले झंडे उठाए चलती थी—जो कर्बला के ग़म का निशान थे। उन्हें ईरानी, अरब और ग़रीबों का साथ मिला।
749 ईस्वी में अबू अल-अब्बास अल-सफ़्फ़ाह (र.ह.) को कूफ़ा में नया ख़लीफ़ा घोषित किया गया। एक साल बाद आख़िरी उमय्यद ख़लीफ़ा मर्वान II को हरा दिया गया। अब्बासी सत्ता आई, मगर बदले की भावना में उन्होंने उमय्यद परिवार के ज़्यादातर मर्दों को क़त्ल कर दिया। बस एक, अब्दुर्रहमान I, स्पेन भागकर बच गए और वहाँ एक नई उमय्यद हुकूमत कायम की जो इल्म, फन और तहज़ीब में चमकी।
अब्बासी सत्ता ने भी अहल-ए-बैत से किया वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने हुसैन (र.अ.) के नाम पर सत्ता ली, मगर बाद में अली के वंशजों को जेल में डाला, ज़हर दिया, और डराया। ज़ुल्म बदला, ज़ालिम बदल गए।
धीरे-धीरे शिया इस्लाम एक संगठित मज़हबी सोच बन गया। अब यह सिर्फ अहल-ए-बैत से मोहब्बत नहीं रही, बल्कि एक पूरा मज़हबी नज़रिया बन गया। शिया मानते हैं कि सिर्फ अली के वंशजों को हक़ है उम्मत की रहनुमाई का। कर्बला की याद और इमामों की अज़मत शिया पहचान का केंद्र बन गई। इससे शिया समाज एकजुट रहा और अलग भी।
शिया इस्लाम के अंदर कुछ ग़ुलात (अत्यधिक मानने वाले) भी हुए, जिन्होंने इमामों को अलौकिक दर्जा दिया। इन विचारों ने शिया इस्लाम को और विविध और सुन्नी इस्लाम से अलग बनाया।
जहाँ सुन्नी बहुसंख्यक ख़लीफ़ा को उम्मत की रज़ामंदी से चुनना मानते हैं, वहीं शिया मानते हैं कि सिर्फ पैग़ंबर (स.अ.) के परिवार का इमाम ही रहनुमा हो सकता है। यह फर्क सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि इंसाफ़ और हक़ की समझ को भी तय करता है।
1501 में ईरान में सफ़वी सल्तनत शुरू हुई। इस्माईल I नाम के 14 साल के युवा ने बादशाह बनते ही शिया इस्लाम को राज्यधर्म बना दिया। उन्होंने ईरान को एक मज़बूत देश बनाया और फ़ारसी तहज़ीब, हुस्न और हूनर को उभारा। सफ़वी सल्तनत 200 साल से ज़्यादा चली और आज के ईरान पर उसका गहरा असर है।
शिया इस्लाम के उलेमा (धार्मिक विद्वान) सफ़वी दौर में बहुत ताक़तवर बन गए। उन्होंने न सिर्फ धर्म बल्कि अदालत और तालीम में भी अहम भूमिका निभाई। वे धार्मिक टैक्स लेते थे और सरकार से आज़ाद होकर काम करते थे। शिया मानते हैं कि जब तक नबी (स.अ.) या गायब इमाम नहीं लौटते, तब तक उलेमा ही समाज की रहनुमाई करेंगे।
कर्बला की रूह ने गूंगे लोगों को आवाज़ दी। 1979 की ईरानी क्रांति में आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने हुसैन (र.अ.) की मिसाल से करोड़ों को उठाया। अली शरीअती ने कहा: “हर दिन आशूरा है, हर ज़मीन कर्बला है”—यानी सच्चाई की जंग कभी खत्म नहीं होती। ख़ुमैनी ईरान के पहले रहबर बने—एक इंसाफ़पसंद, मज़बूत और धार्मिक रहनुमा।
कर्बला की बाद की कहानी सिर्फ आंसुओं की नहीं थी। यह पहचान, प्रतिरोध, याद और हक़ का सफ़र था। इमाम हुसैन (र.अ.) की शहादत बेकार नहीं गई। उन्होंने एक जज़्बा दिया—उम्मीद, हिम्मत और सच्चाई का। आज भी, चाहे शिया हो या सुन्नी—जो भी इंसाफ़ चाहता है, उसके दिल में कर्बला की चोट महसूस होती है। कर्बला सिखाती है: ताक़त अगर हक़ के बिना हो, तो बेकार है। और असली जीत ज़िंदा रहने में नहीं, बल्कि हक़ के लिए डट जाने में है—चाहे जान चली जाए।
डॉ. उज्मा खातून
इस्लामी अध्ययन विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षिका रह चुकी हैं।