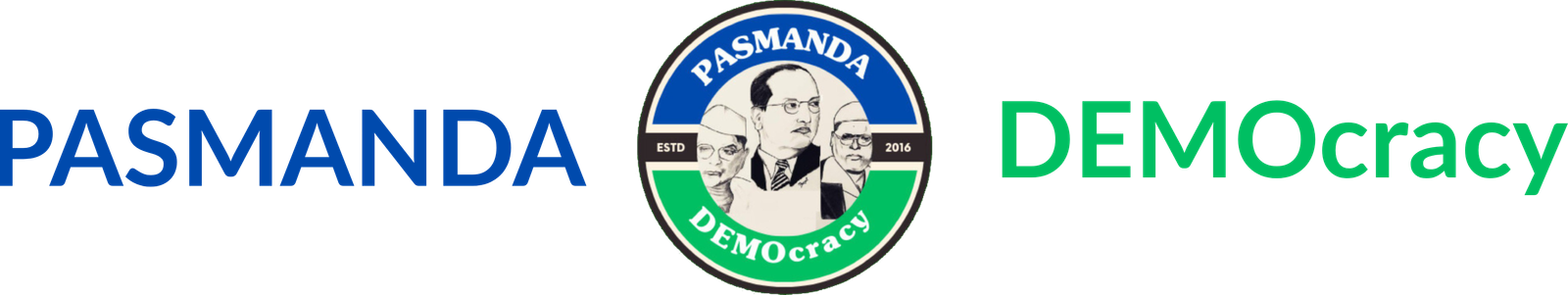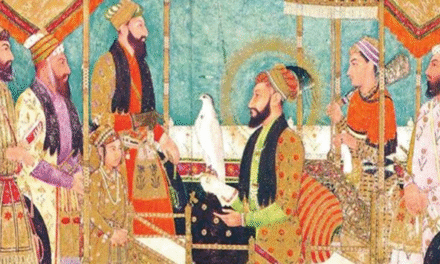लेखक: अब्दुल्लाह मंसूर
हम सब कभी न कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं—हमारे जीवन का मकसद क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? इन सवालों का जवाब हमें विज्ञान की किताबों में नहीं मिलता। विज्ञान हमें बताता है कि दुनिया ‘कैसे’ चलती है, जैसे बारिश कैसे होती है या हमारा शरीर कैसे काम करता है। लेकिन विज्ञान यह नहीं बताता कि हमें जीवन ‘क्यों’ जीना चाहिए। यहीं पर एक ‘अर्थ-प्रणाली’ की आवश्यकता महसूस होती है, चाहे वह धर्म हो, दर्शन हो, या कोई नैतिक विचारधारा। यह हमारे जीवन के उन खाली कोनों को भरती है, जहाँ सिर्फ़ तथ्य और तर्क अधूरे रह जाते हैं।
विज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रकृति मानवीय भावनाओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाती। विज्ञान के लिए प्रेम, करुणा, या उम्मीद जैसी भावनाएँ दिमागी गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक इंसान के लिए ये उसके जीवन का सार हैं। मुश्किल के समय में, हमें वैज्ञानिक तथ्यों से ज़्यादा भावनात्मक सहारे और उम्मीद की ज़रूरत होती है। यहीं पर आस्था जैसी प्रणालियाँ हमें सहारा देती हैं। यह विश्वास दिलाती है कि हमारे अस्तित्व का कोई वृहत्तर उद्देश्य है, जिससे हमें अनिश्चितता और अकेलेपन से लड़ने की हिम्मत मिलती है।
इसके ठीक विपरीत एक दर्शन है जिसे ‘शून्यवाद’ (Nihilism) कहते हैं। यह दर्शन मानता है कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ, मूल्य या उद्देश्य नहीं है। यह सोच इंसान को गहरी निराशा और उद्देश्यहीनता की ओर ले जाती है। अगर कुछ भी मायने नहीं रखता, तो जीने या कुछ भी बेहतर करने की प्रेरणा ही खत्म हो सकती है। यह एक नैतिक शून्य पैदा करता है, जहाँ सही और गलत के बीच का फ़र्क़ मिट जाता है। कोई भी सार्थक समाज इस शून्य पर खड़ा नहीं हो सकता।
हालांकि, यह भी सच है कि धर्म का एक स्याह पहलू भी है। इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर अनगिनत युद्ध, हिंसा और नफ़रत फैलाई गई है। इस पर लगातार बात होती है और होनी भी चाहिए। ज़्यादातर युद्धों के पीछे सत्ता, ज़मीन और संसाधनों का लालच रहा है, जहाँ धर्म को केवल एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हिटलर या मुसोलिनी की विचारधारा किसी धर्म से प्रेरित नहीं थी। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि धर्मग्रंथों की संकीर्ण और कट्टर व्याख्याओं ने भी अक्सर घृणा को वैचारिक आधार दिया है।
हाल के दिनों में, कुछ ‘नव-नास्तिक’ (New Atheist) विचारकों, जैसे सैम हैरिस, की आलोचना में इस्लामोफोबिया का एक तत्व देखा गया है, जहाँ इस्लाम को विशेष रूप से हिंसक बताया जाता है। यह एक सरलीकृत और खतरनाक दृष्टिकोण है जो ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा करता है। यह इस्लामी सभ्यता के दर्शन, विज्ञान और गणित में दिए गए असाधारण योगदान को नज़रअंदाज़ करता है और एक ऐसी साम्राज्यवादी सोच को बढ़ावा देता है जो पश्चिम को “सभ्य” और बाकी दुनिया को “अज्ञानी” के रूप में देखती है।
असल समस्या धर्म या विज्ञान में नहीं, बल्कि उनके सत्ता और पूंजी के हाथों का उपकरण बन जाने में है। विज्ञान ने हमें परमाणु ऊर्जा की समझ दी, लेकिन सत्ता के लालच ने उससे परमाणु बम बनवाए। ऑटोमेशन ने हमें उत्पादन की असीम क्षमता दी, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के मुनाफ़े की होड़ ने करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। विज्ञान एक शक्तिशाली औज़ार है; इसका उपयोग मानवता के लिए होगा या विनाश के लिए, यह हमारे नैतिक विवेक पर निर्भर करता है।
यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि नैतिकता और उद्देश्य के लिए किसी एक निर्माता ईश्वर में विश्वास करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद (Secular Humanism) एक शक्तिशाली दर्शन है जो तर्क, करुणा और मानवीय मूल्यों को नैतिकता का आधार मानता है। इसी तरह, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कन्फ्यूशीवाद जैसी प्राचीन प्रणालियों में ईश्वर की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, फिर भी इन सभ्यताओं ने दुनिया को गहरे नैतिक सिद्धांत दिए हैं। इसका सार यह है कि एक मज़बूत नैतिक ढाँचा, चाहे वह ईश्वर पर केंद्रित हो या मानवता पर, समाज को जोड़ने और उसे बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है।
जीवन की यात्रा में विज्ञान और विवेकपूर्ण आस्था विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री हैं। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के ‘कैसे’ को समझने की शक्ति और साधन देता है, जबकि एक नैतिक प्रणाली हमें जीवन के ‘क्यों’ का बोध कराती है—उद्देश्य, करुणा और न्याय। इतिहास गवाह है कि जब भी विज्ञान को नैतिकता से या आस्था को विवेक से अलग किया गया, परिणाम विनाशकारी हुए।
एक संतुलित और मानवीय भविष्य का मार्ग न तो कोरे भौतिकवाद में है, न ही तर्कहीन अंधविश्वास में। असली चुनौती विज्ञान की तर्कसंगत खोज को आस्था और मानवतावाद के नैतिक प्रकाश के साथ जोड़ने में है। जब हम ज्ञान की शक्ति को करुणा के उद्देश्य से मिला देते हैं, तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो, बल्कि सार्थक, empathic और न्यायपूर्ण भी हो।
अब्दुल्लाह मंसूर, एक लेखक और पसमांदा बुद्धिजीवी हैं। वे ‘पसमांदा दृष्टिकोण’ से लिखते हुए, मुस्लिम समाज में जाति के प्रश्न और सामाजिक न्याय पर केंद्रित हैं